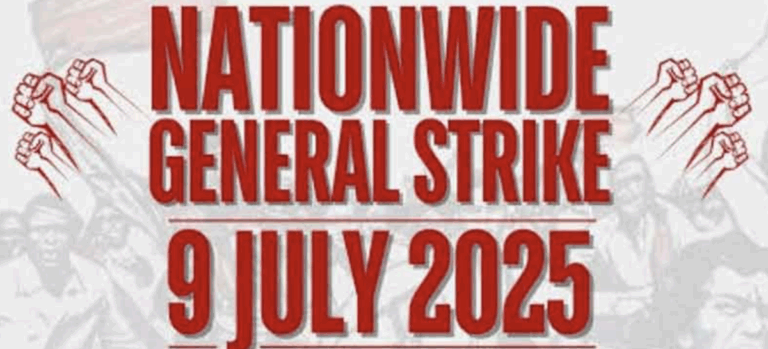आमतौर पर वोट के समीकरण बैठाने के संदर्भ में गठबंधन की राजनीति की व्याख्या करने का रिवाज राजनीतिक चिंतकों में पिछले दो दशकों से बढ़ा है। यह मान लिया जाता है कि गठबंधन में शामिल पार्टियों का अलग-अलग वोट प्रतिशत स्थिर रहेगा और गठबंधन के समीकरण में यह उसी मात्रा में एक दूसरे से जुड़ जाएगा। लेकिन चुनाव के परिणाम यह दिखाते हैं कि इस तरह का समीकरण होता नहीं हैं। यह सिर्फ अवधारणा है।
चुनाव के परिणाम को निर्णायक तरीके से बदल देने को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर एक सफल गठबंधन 1977 में जनता पार्टी के रूप में सामने आया था। इसके अगुआ जयप्रकाश नारायण थे। यह आपातकाल और इंदिरा गांधी की तानाशाही भरे राज के खिलाफ बनाया गया गठबंधन था। इस गठबंधन में कई राजनीतिक धाराएं, जिसमें 1967 के दौर में उभरकर आये कई क्षेत्रीय दल शामिल थे, अपनी पहचान को इसमें मिला देने का निर्णय लिया था। कारण, देश और लोकतंत्र को बचाना था।
इस गठबंधन में दो ऐसी धाराएं थीं जिनकी पहचान अखिल भारतीय स्तर की थीं; यद्यपि चुनाव में उन्हें हासिल नतीजे नाममात्र के ही होते थे। इसमें एक समाजवादियों की धारा थी और दूसरी जनसंघ थी। 1977 के आम चुनावों में जनता पार्टी को 41.32 प्रतिशत वोट मिले थे जबकि कांग्रेस को 34.52 प्रतिशत। लगभग 7 प्रतिशत वोट का ही फर्क था लेकिन सीट की संख्या में काफी फर्क आ गया था। जनता पार्टी को 295 और कांग्रेस को 154 सीटें मिली थीं।
1980 तक आते-आते यह गठबंधन बिखर चुका था और इसमें शामिल पार्टियां अपने-अपने जनाधारों की ओर बढ़ गईं। एक बार फिर क्षेत्रीय दलों का दौर सामने आया। इन दलों के पास क्षेत्रीय पकड़ और आम चुनावों का अनुभव बन चुका था। यह भी स्पष्ट था कि कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका अखिल भारतीय चरित्र हो। कांग्रेस को भी यह अहसास हो चुका था कि उसके वोट का आधार दरक चुका है। और क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक संबंध बनाकर चले बिना आगे जाने का रास्ता कठिन है।
1980 के आम चुनावों में कांग्रेस 42 प्रतिशत से अधिक वोट के साथ वापसी कर चुकी थी लेकिन यही वह समय था जब बसपा और भाजपा जैसी पार्टियों की नींव पड़ रही थी। और साथ ही टूट के बाद भी बची रह गई जनता पार्टी के दो धड़ों के वोट का कुल योग लगभग 28 प्रतिशत था।
यहां यह ध्यान रखना होगा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसी दौर में राष्ट्रवाद का हिंदूवादी पुनर्गठन तेजी से हो रहा था और यह हिंदी पट्टी को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। हिंदू राष्ट्रवाद की संवेदनशीलता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस कदर बढ़ी उसका परिणाम कांग्रेस को ऐतिहासिक वोट और सीट की बढ़त में मिला। कांग्रेस की विशाल बहुमत की राष्ट्रवादी संवेदनशीलता 1988 तक आते-आते बिखरने लगी। सामाजिक संरचना में बढ़ती नई गोलबंदी वोट और सत्ता पर दावेदारी कर रही थी और भारतीय राज्य के अंतर्विरोधों के साथ उलझ रही थी।
1989 में एक बार फिर चुनाव में वोट के नजरिये से वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल और भाजपा के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से सरकार बनाई गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 39.53 प्रतिशत वोट मिला था लेकिन सीट की संख्या 197 पर टिक गई। जबकि विपक्ष की जीती हुई मुख्य पार्टियों का कुल वोट जोड़ दें, तब भी उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस से नीचे ही था। जबकि जनता दल, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों धड़ों की जीत का कुल योग से संसद में सरकार बनाने का बहुमत आ गया था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा के सामने सामाजिक गोलबंदी और राजनीतिक अंतर्विरोधों से उलझने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया और इससे टकराने के बाद यह एक बार फिर बिखर गया।
सामाजिक न्याय और हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद के बीच की टकराहट और संतुलन बनाने का नायाब काम नरसिम्हा राव की कांग्रेस ने किया और भारतीय राजनीति से मुस्लिम प्रतिनिधित्व को अलविदा कर दिया। ऐसे में भाजपा के सामने बसपा का दामन पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम के मजबूत जनाधार को एकदम ही छोड़ दिया। यहां से कांग्रेस अपने राज्यों के नेतृत्व पर जोर देते हुए क्षेत्रीय राजनीति के समीकरण की ओर बढ़ गई। यह रणनीति कांग्रेस की आगामी गठबंधन की राजनीति का आधार भी था।
जबकि भाजपा राजनीतिक सांस्कृतीकरण के रास्ते दलित, ओबीसी और अन्य समुदायों को अपना हिस्सा बनाने की ओर गई। कांग्रेस को 35.66 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कम्युनिस्ट पार्टी और कई बार विपक्ष की भाजपा सरकार के समर्थन से कांग्रेस की सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा कर गई। 1996 के चुनाव में कांग्रेस के वोट प्रतिशत के अनुपात में सीटों की संख्या और अधिक गिरी। भाजपा के वोट प्रतिशत में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हुई और उसने सरकार बनाने का दावा किया लेकिन वह सफल नहीं रहा।
कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों की आकांक्षा और किसानों में से उभरे संप्रभु वर्ग को सामाजिक न्याय के नाम पर तरजीह देना बेहतर समझा। एक बार सरकार बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा को सामने लाया गया और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री चुने गये। 1998-99 में भाजपा ने चुनाव के मद्देनजर एनडीए का गठन किया। इससे कांग्रेस के वोट प्रतिशत में महज डेढ़ प्रतिशत की गिरावट आई। भाजपा को वोट प्रतिशत में मामूली बढ़त मिली। लेकिन गठबंधन की पार्टियों के समर्थन से भाजपा केंद्र पर पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने में कामयाब रही।
यदि हम गठबंधन की राजनीति से वोट प्रतिशत में बढ़ोत्तरी का आंकड़ा देखें, तो इसमें नेतृत्व करने वाली पार्टियों को सीधा फायदा होता नहीं दिखता है। इसमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक तौर पर उभरकर आते हुए दिखती है। जब भी भाजपा और कांग्रेस का वर्चस्व इन पार्टियों पर बढ़ा है, गठबंधन में टूट की स्थिति भी बनी है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात सामाजिक न्याय और जनाधार का दावा है।
1990 के बाद उभरी राजनीति में मुसलमान को भारतीय राजनीति के एजेंडे से बाहर करने की ओर ले जाया गया। वहीं, दलित समुदाय का ब्राह्मणवादी सांस्कृतीकरण कर उसे हिंदूत्व की धारा में लाने की प्रक्रिया पर हिंसक तरीके से जोर दिया गया। यही स्थिति आदिवासी समुदाय के साथ भी बनाई गई। इसके लिए इन जनाधारों को नई पाटियों का गठन कर या कराकर उन पार्टियों को अस्तित्व के संकट में डाल दिया गया जो इन जनाधारों पर एकतरफा दावा करती थीं। भाजपा अपनी राजनीति और विचारधारा में इस तरह के कार्यों में काफी दूर तक आगे गई। 2002 में मोदी के नेतृत्व में उभरा गुजरात माॅडल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति को महज एक मुखौटा बना दिया। दरअसल, भाजपा को इसकी जरूरत नहीं रह गई।
कांग्रेस के नेतृत्व में 2024 के चुनाव के मद्देनजर जो गठबंधन सामने आया है, उसमें उसका नाम बदल जाना उपयुक्त ही है। यह गठबंधन यूपीए की संरचना से एकदम अलग है और इसमें शामिल कई मुख्य पार्टियां भाजपा के गठबंधन का हिस्सा रही हैं। इस गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की प्रधानता है जबकि भाजपा जिस गठबंधन पर काम कर रही है वहां वोट की कथित सोशल इंजीनियरिंग है।
आंकड़े बताते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग से वोट के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी मामूली स्तर की ही होती है। गठबंधन की राजनीति में केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना और उसके नेतृत्व की तानाशाही और असफलता ही मुख्य एजेंडा होता है। इसी जमीन पर क्षेत्रीय दलों की स्थिति मजबूत होती है और केंद्र में बदलाव की दावेदारी भी असर डालती है। कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन इस काम को किस दूर तक ले जायेगा, यह आने वाला समय ही बतायेगा।
भारत में होने वाले आम चुनाव राजसत्ता के मूल चरित्र में कोई फर्क नहीं लाते हैं। लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यावादी राजनीति के हिंदुत्व के फासीवादी बहुसंख्यावाद में बदल जाने की ओर बढ़ना यह दिखा रहा है कि इसमें से मुसलमान, दलित, आदिवासी और मेहनतकश, खासकर मजदूर और किसान बाहर की ओर धकेल दिये गये हैं। केंद्र की भाजपा सरकार रिजर्व बैंक की नीतियों के माध्यम से नोटबंदी और फिर 2000 रुपये की नोटबंदी कर वित्त पूंजी के खिलाड़ियों को मजबूत कर रही है, यहां तक कि इन वित्तीय संसाधनों पर सट्टेबाजी और अय्याशी करने वालों को छूट दी जा रही है।
वित्तीय घपलों के अपराधियों और भगोड़ों को शुद्ध-साफ करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। दूसरी ओर बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों को निवेश के नाम पर ऐसे उद्योगों को ले आया जा रहा है जिसमें भारत के पूंजीपति महज असेंबलिंग का काम करेंगे। रेलवे, पोर्ट, पब्लिक सेक्टर और यहां तक कि बैंकों का जिस तरह निजीकरण हो रहा है, उससे भारत की कुल स्थायी पूंजी में तेजी से गिरावट आ रही है।
मुद्रास्फीति की दर बढ़ाकर बाजार में जरूरी सामानों के दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति अब एक स्थाई रूप ले रही है। ये वे मुख्य आर्थिक आधार हैं जिस पर भाजपा खड़ी है और इनकी राजनीति कर रही है। इसी आधार पर भाजपा की केंद्र सरकार को विदेशी हुक्मरानों से समर्थन और तारीफें मिल रही हैं। इस संदर्भ में हम भारत की राजसत्ता के चरित्र में आ रहे बदलाव को हम देख सकते हैं और इससे उपजने वाले संकट को समझ भी सकते हैं।
आज के समय में एक कवि के शब्दों में: बस इतना ही मिल जाये-
मुझे साफ पानी और
कम क्रूरता वाला शहर चाहिए जहां
अगर कोई हमला करने आए तो बचाने के
लिए बगल वाला आए। यह न आए तो उसके
बगल वाला आए और अगर वह भी न आए तो
पूरे शहर में चर्चा शुरू हो जाए कि देखो
आजकल आदमी को बचाने आदमी कैसे नहीं
आता।
सच्चाई तो यही है; इसी कवि के शब्दों में: ‘मुझे ऐसा शहर नहीं चाहिए जहां रामदास को/ मालूम हो कि रामदास की हत्या होगी।’ इस भयावह परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति अपने जनाधारों के साथ किस तरह का रिश्ता बनाती है और क्या परिणाम लेकर आयेगी, इसे तो जरूर ही देखना बाकी है।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)