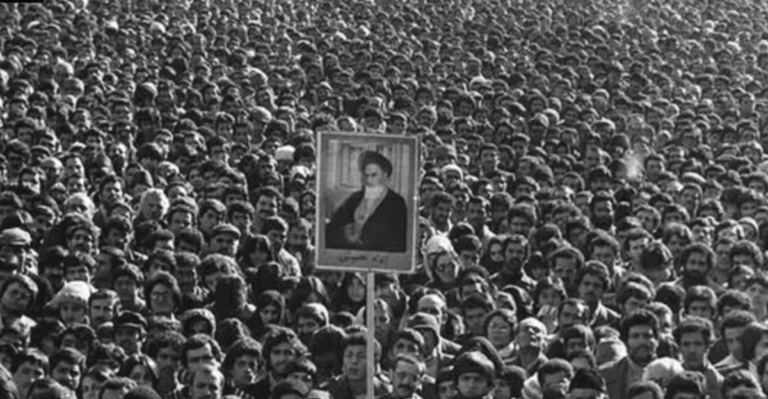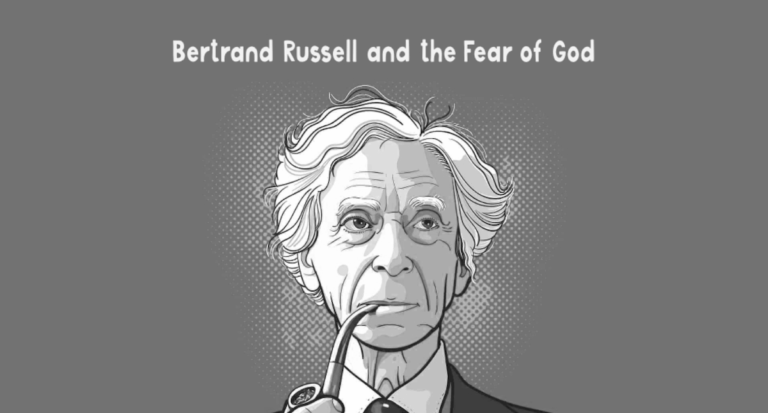भाषा की कोपलें किसी आदेश या दबाव से नहीं फूटतीं, वह मनुष्य के विचार, अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक चेतना से उपजती है। जैसे जल बहता है, वैसे ही भाषा स्वाभाविक, सहज, बिना किसी कृत्रिम बंधन के बहती है। जब किसी भाषा को दूसरी पर थोपा जाता है, तो यह केवल भाषाई अन्याय ही नहीं होता, इससे सांस्कृतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का भी दमन होता है। यही बात आज महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर मराठी भाषा के जबरन थोपे जाने के संदर्भ में गंभीरता से समझी जानी चाहिए।
मराठी बनाम हिंदी नहीं, भाषाई समरसता बनाम भाषाई थोप
बहुभाषी भारत में हर भाषा अपने भूगोल, इतिहास और जनभावनाओं से जुड़ी हुई है। मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है, जैसे कि हिंदी उत्तर भारत की रूह है। लेकिन, जब एक क्षेत्र में किसी दूसरी भाषा बोलने वालों पर स्कूलों, सरकारी नौकरियों या रोज़मर्रा के लेन-देन में क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य किया जाता है, तो यह भाषाई गर्व नहीं, भाषाई अधिनायकवाद बन जाता है।
महाराष्ट्र के कई शहरों में अब हिंदी भाषियों को यह कहकर धमकाया जा रहा है कि “यहां रहना है, तो मराठी बोलो।” यह उस सांस्कृतिक समरसता के खिलाफ है, जिसने मुंबई को एक वैश्विक महानगर और महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील राज्य बनाया है। क्या यह संभव है कि कोई दिल्ली में मराठी बोलने पर दंडित हो ? क्या कोलकाता में तमिल बोलने वालों को कोई अपमानित करता है ? नहीं। क्योंकि भाषाएं हमारी संकीर्णता का नहीं, विविधता का प्रमाण हैं।
भाषा का विकास प्रतिबंधों से नहीं, विचारों से होता है
भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों का भी वाहक है। जब कोई व्यक्ति सोचता है, तब वह भाषा में ही सोचता है- वही भाषा उसकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, कलात्मक दृष्टि को आकार देती है। जब उस पर कोई दूसरी भाषा थोपी जाती है, तो केवल शब्द नहीं बदलता, बल्कि उसकी सोचने की स्वतंत्रता पर आघात होता है।
मराठी एक समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा वाली भाषा है। लेकिन, उसकी महानता इस बात में नहीं है कि वह दूसरों पर थोप दी जाए, बल्कि इस बात में है कि वह खुद में इतनी जीवंत, विचारशील और रचनात्मक बने कि लोग स्वेच्छा से उसे सीखने और अपनाने को प्रेरित हों। हिंदी, तमिल, बंगाली, या उर्दू- कोई भी भाषा अगर थोप दी जाए, तो उसका सौंदर्य दम घुटने लगता है।
राजभाषा, मातृभाषा और संवैधानिक अधिकार
भारत के संविधान ने हर नागरिक को अपनी मातृभाषा में सोचने, पढ़ने, लिखने और बोलने का अधिकार दिया है। राज्यों को भी अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। लेकिन, जब राज्य के भीतर भाषायी अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है, उनके स्कूलों पर मराठी अनिवार्य की जाती है, उनकी नौकरियों में भाषाई शर्तें लगाई जाती हैं, तो ऐसा करने से संवैधानिक मूल्यों की हत्या होती है।
महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की एक बड़ी संख्या है, जो दशकों से वहां रह रही है; वे राज्य के विकास में सहभागी रहे हैं, टैक्स देते हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षा में योगदान करते हैं। क्या केवल भाषा के आधार पर उनकी भागीदारी को सीमित करना न्यायोचित है?
क्या भाषा प्रेम, बहिष्कार से आता है?
अगर कोई यह सोचता है कि हिंदी भाषियों को मराठी पढ़ने पर मजबूर कर देने से मराठी का उत्थान हो जाएगा, तो यह दृष्टिकोण न केवल अधूरा है, बल्कि आत्मघाती भी है। भाषा तभी पढ़ी जाती है, जब वह आकर्षित करती है; भाषा तभी बोली जाती है, जब वह अपनाई जाती है। जबरन पढ़ाने और बोलवाने से लोग उस भाषा के प्रति विरोधी रुख अपना लेते हैं। यह एक सामाजिक प्रतिकार की स्थिति उत्पन्न करता है।
बहुभाषिकता भारत की दुर्बलता नहीं, शक्ति है
भाषा नदियों की तरह हैं, जो अपनी-अपनी दिशाओं में बहती हैं, पर समंदर में मिलती हैं। हिंदी और मराठी एक-दूसरे की विरोधी नहीं, पूरक भाषाएं हैं। मराठी की प्रगति हिंदी को दबाकर नहीं होगी, बल्कि तब होगी जब मराठी समाज उसे विचारों, लेखन और नवाचार की भाषा बनाए रखेगा।
राज्य सरकारों और भाषायी संगठनों को यह समझना होगा कि भाषा का गौरव उसे थोपने से नहीं, उसे जीवंत रखने से आता है। मराठी का सम्मान तभी बढ़ेगा, जब वह अहंकार नहीं, आत्मीयता का माध्यम बनेगी।
(उपेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं।)