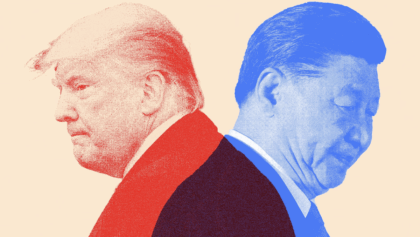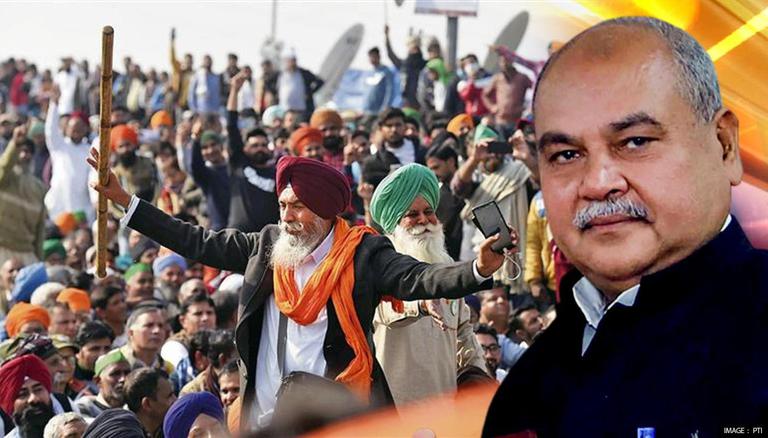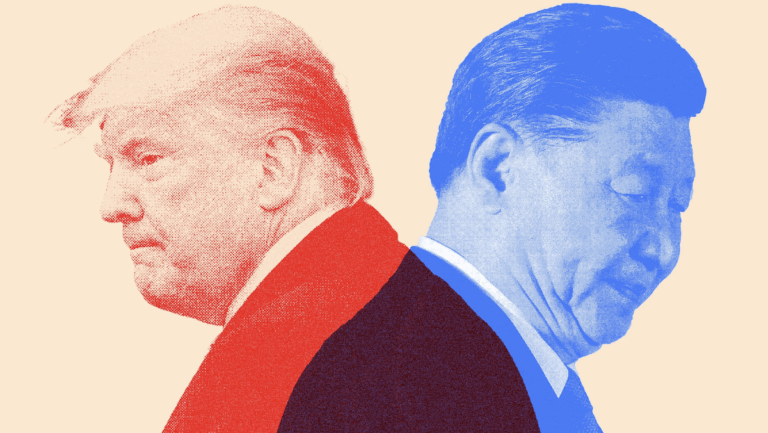बहुत प्रयास करने के बाद भी किसान आंदोलन की सफलता के जश्न में शामिल न हो पाया। सिर्फ इतना ही नहीं जश्न मना रहे किसान नेताओं और बुद्धिजीवियों को कौतूहल, आश्चर्य एवं करुणा मिश्रित दृष्टि से देखता भी रहा। अपने हृदय में झांका तो वहाँ क्षोभ एवं संशय की उपस्थिति देख खुद पर क्रोध आया। आखिर इसका कारण क्या था?
भारत की अर्थनीति, विकास प्रक्रिया और आधुनिक राजनीति का कोई अति सामान्य छात्र भी यह अनुमान लगा सकता है कि तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सरकार ने उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत कुछ राज्यों में निकट भविष्य में होने वाले चुनावों के मद्देनजर लिया है। सरकार किसानों की नाराजगी से डरी हुई है और इसी कारण चुनावों तक वह इस मुद्दे को शांत रखना चाहती है।
लेकिन सरकार इस बात पर अडिग है कि उसका फैसला देश और विशेषकर किसानों के हित में है और इन सुधारों के अतिरिक्त कृषि और कृषकों की दशा सुधारने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तब उन्होंने देश से इस बात के लिए क्षमा मांगी कि इन लाभकारी कृषि कानूनों की प्रकट और स्पष्ट महत्ता को किसानों के एक वर्ग को समझा पाने में सरकार असफल रही और इस कारण उसे कानून वापसी का निर्णय लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहीं नहीं कहा कि कानून किसान विरोधी हैं बल्कि उन्होंने कहा कि इन किसान हितैषी कानूनों की उपयोगिता को लोगों तक कम्यूनिकेट करने में वे नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा-“साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य, कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए।”
प्रधानमंत्री के इन शब्दों में सरकार की भावी रणनीति के संकेत छिपे हैं। आने वाले समय में सरकारी प्रचार तंत्र और सरकार समर्थक मुख्यधारा के मीडिया का उपयोग यह प्रदर्शित करने हेतु किया जाएगा कि यह कानून लाभकारी हैं और इनकी उपयोगिता को देश के नागरिक तथा अधिसंख्य किसान समझ भी रहे हैं। इस प्रकार पुनः आंदोलनरत किसानों को मुट्ठी भर नासमझ किसानों के रूप में प्रस्तुत करने का अभियान नए तेवर और कलेवर में प्रारंभ करने की सरकार की तैयारी है।
आंदोलनरत किसानों का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ है और वे अभी ठीक से अपने घरों तक पहुंच भी नहीं पाए हैं ऐसे समय में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सरकार की भावी रणनीति के विषय में वही कहा है जिसका संकेत कृषि कानूनों की वापसी का एलान करते समय प्रधानमंत्री ने दिया था, तोमर ने कहा-“कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म था। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा।” उन्होंने आगे कहा कि “हम एक कदम पीछे जरूर हटे हैं। लेकिन दोबारा आगे बढ़ेंगे। सरकार आगे के बारे में सोच रही है, हम निराश नहीं हैं। किसान भारत की रीढ़ हैं।”
विश्व की अर्थव्यवस्था तथा कृषि एवं व्यापार को नियंत्रित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं विकसित देशों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे सरकार पर वर्षों से दबाव डालती रही हैं कि कृषि को बाजार के हवाले कर दिया जाए। उनकी दृष्टि में यह कृषि कानून भारतीय कृषि को विश्व बाजार और मुक्त अर्थव्यवस्था के लिए खोलने का पहला सकारात्मक प्रयास हैं। यह सरकार इतनी दृढ़ और स्वाभिमानी तो कतई नहीं है कि वह इस अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना कर सके।
सत्तारूढ़ दल को वित्तपोषित करने वाले मित्र कॉरपोरेट घरानों ने कृषि कानूनों के लागू होने की प्रत्याशा में बहुत सी अग्रिम तैयारियां कर ली थीं कि इन कृषि कानूनों के प्रभावी होने के बाद भारत की कृषि को वे किस प्रकार अपने कब्जे में लेंगे। इन कानूनों को वापस लेने के सरकार के निर्णय से उन्हें अवश्य झटका लगा होगा। उनकी नाराजगी दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी।
इन सारी परिस्थितियों के मद्देनजर यह लगभग स्पष्ट था कि सरकार इन कानूनों को किसी अन्य विधि से प्रच्छन्न रूप से अवश्य लाने का प्रयास करेगी। कानून वापसी का सरकार का निर्णय समय निकालने की, चुनावों में नुकसान कम करने की, स्वयं को लोकतांत्रिक सिद्ध करने की और चुनावों में सफलता मिलने पर किसान आंदोलन पर नए सिरे से आक्रमण करने की सुविचारित रणनीति का एक हिस्सा है।
किसान अपनी दूसरी प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के विषय में भी सरकार से कोई स्पष्ट घोषणा कराने में सफल नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार खेती के तौर-तरीकों में परिवर्तन लाने तथा एमएसपी को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। जिस समिति का निर्माण होना है उसमें होने वाली चर्चा उस दशकों पुरानी स्थापना के इर्दगिर्द ही केंद्रित रहेगी जिसके अनुसार किसानों को एमएसपी देना देश की अर्थव्यवस्था और आम उपभोक्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा फिर भी दयालु सरकार अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और जो कुछ भी निर्णय लिया जाए वह देशहित और सरकार की आर्थिक मजबूरियों को ध्यान में रखकर लिया जाए।
फिर यह समिति केवल एमएसपी के मामले को ही नहीं देखेगी अपितु यह कृषि की बेहतरी से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार करेगी। कुल मिलाकर विमर्श और विवाद तथा आरोप-प्रत्यारोप का एक अंतहीन सिलसिला चल निकलेगा। होना तो यह था कि सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की घोषणा करती और समिति इस बात के लिए बनती कि इसका क्रियान्वयन कैसे हो?
इसके बावजूद किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। देश में पहली बार ऐसी स्थिति बन रही थी कि चुनाव किसान के मुद्दे पर, उसकी समस्याओं और मांगों पर केंद्रित होने जा रहे थे। आंदोलन के स्थगित होने ने राजनीतिक दलों को यह अवसर दिया है कि वे किसानों को यह स्मरण दिलाएं कि वे पहले जाति-धर्म और क्षेत्र के आधार पर मतदान करते रहे हैं और इस बार भी उन्हें ऐसा ही करना है।
खेती को हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने का प्रयास आसान नहीं है- यह वर्तमान विकास प्रक्रिया को रोकने और उलटी दिशा में चलाने की कठिन कवायद है। जैसे मुद्दों को किसान आंदोलन स्पर्श करता है वैसे मुद्दों पर आधारित आंदोलन लंबे चलते हैं। ये आंदोलन थकते भी हैं, रुकते भी हैं, विश्राम भी करते हैं और नई ऊर्जा के साथ फिर प्रारंभ हो जाते हैं। क्या किसान आंदोलन का स्थगन शक्ति अर्जित करने के लिए लिया गया रणनीतिक युद्ध विराम है। आंदोलन के स्थगन के बाद चल रहा घटनाक्रम इस बात की पुष्टि नहीं करता।
अनेक किसान संगठन चुनावी राजनीति में खुलकर (नव गठित दल के रूप में, किसी राजनीतिक दल के सहयोगी के रूप में या उस राजनीतिक दल में सम्मिलित होकर अथवा किसी मोर्चे का भाग बनकर) हिस्सा लेना चाहते हैं। काश हमारा जीवन उन फिल्मों की भांति सरल होता जिनमें आंदोलनकारी थोड़ी जद्दोजहद के बाद व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन में कामयाब हो जाते हैं, जनता उनका वैसा ही स्वागत करती है जैसा उन जैसे नायकों का होना चाहिए। वे सत्तारूढ़ होते हैं। इसके बाद उनके राज्य में सदैव सुख शांति बनी रहती है।
आंदोलन की प्रकृति में सत्ता से दूरी बनाकर रखना और सत्ता विरोध जैसी विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं। आंदोलन सत्ता को निरंकुश होने से रोकते हैं और न केवल सत्ताधारी दल को बल्कि जनता से कट चुके विरोधी दलों को भी जनाकांक्षाओं से अवगत कराते हैं, उन्हें जनाक्रोश की शक्ति का बोध कराते हैं। जब आंदोलन सत्ता प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तब विजय सत्ता की ही होती है। भले ही आंदोलनकारी ही सत्ता में क्यों न आ जाएं, सत्ता प्राप्त करने की उठापटक ही उन्हें आंदोलन के मूल उद्देश्य से भटका देती है और फिर सत्ता में आने के बाद वे पूरी तरह इसके रंग में रंग जाते हैं।
इतिहास गवाह है कि जनता अनेक बार आंदोलनकारियों को चुनावों में नकार देती है क्योंकि जनता ने उन्हें संघर्ष के लिए चुना होता है, शासन के लिए नहीं। आंदोलनकारियों की चुनावी असफलता के कुछ स्थूल कारण भी होते हैं-बिना तैयारी के चुनावों में उतरना, जमीनी संगठन का अभाव, धनाभाव आदि। कारण जो भी हो आंदोलनकारियों की चुनावी पराजय की व्याख्या एक ही होती है- आंदोलन के मुद्दों को जनता ने नकार दिया है इसलिए यथास्थिति बनी रहनी चाहिए।
यदि आंदोलनकारी चुनकर सत्ता में आ भी जाते हैं- जैसे क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीति करने वाली असम गण परिषद या झारखंड मुक्ति मोर्चा अथवा जनलोकपाल आंदोलन का अयाचित-अनपेक्षित उत्पाद आम आदमी पार्टी- तब भी धीरे धीरे वे किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की भांति ही अवसरवादी और समझौतापरस्त बन जाते हैं।
पहले यह समझा जा रहा था कि आंदोलित किसानों से समझौता सरकार की मजबूरी है लेकिन हालिया घटनाक्रम तो यह संकेत करता है कि समझौते के लिए किसान नेता भी उतने ही इच्छुक थे जितनी कि सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने घटक किसान संगठनों में से कुछ की चुनावी राजनीति में प्रवेश की इच्छा को जानने के बाद उन्हें यह समझाने की कोशिश की हो कि चुनावी राजनीति में प्रवेश का निर्णय आंदोलन के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक सिद्ध हो सकता है इसलिए उन्हें अपना निर्णय बदलना चाहिए। किंतु उन्हें अपनी जिद पर अडिग पाकर शीर्ष नेतृत्व को यह चिंता सताने लगी हो कि चलते आंदोलन के बीच इस प्रकार के मतभेद गलत संदेश देंगे इसलिए आंदोलन स्थगित करने की पहल की गई।
किसान आंदोलन में कृषि के अलग अलग पक्षों को प्रधानता देने वाले संगठन एवं किसान नेता जुड़े हुए हैं। वाम विचारधारा से प्रभावित किसान नेताओं का वास्तविक संघर्ष भूमिहीन कृषि मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक तथा छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक शक्ति दिलाने के लिए है। समाजवाद से प्रभावित किसान नेता ग्राम और कृषि को सत्ता संचालन में मुख्य स्थान दिलाना चाहते हैं। एक वर्ग सम्पन्न और बड़े पारंपरिक किसानों का है जो कृषि उपज के लाभकारी मूल्य एवं किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए संघर्षरत है। कुछ पर्यावरणवादी भी आंदोलन से जुड़े हैं जो पर्यावरण सम्मत कृषि को केंद्र में रखने और इसे लाभकारी बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं। यह सारी विचारधाराएं कहीं न कहीं आपस में टकराती हैं और कानून वापसी के मुख्य मुद्दे के समाप्त हो जाने के बाद इनके पारस्परिक मतभेदों के सतह पर आने का खतरा बना रहेगा।
किसान आंदोलन की एकजुटता और धैर्य ने सभी को प्रभावित किया था। लगता था कि यह आंदोलन धीरे धीरे न केवल समूचे देश में फैलेगा अपितु इससे मजदूर,छोटे व्यापारी और नौकरीपेशा मध्यम वर्गीय लोग भी जुड़ जाएंगे। निजीकरण, वैश्वीकरण और नगरीकरण जैसी अवधारणाओं को अब चुनौती दी जा सकेगी। कॉरपोरेट के स्थान पर कोऑपरेटिव की चर्चा होगी। अब गांव, खेती और किसान को केंद्र में रखकर देश का संचालन हो सकेगा। गांधी, लोहिया और ज्योति बसु के विचारों का पुनर्पाठ होगा। लगता था कि धर्म और जाति की राजनीति की समाप्ति तथा देश के सेकुलर चरित्र एवं संघात्मक ढांचे की रक्षा का कार्य भी किसान आंदोलन के माध्यम से ही संपन्न होगा।
किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ ज्यादा ही आशावादी हो गए हैं। अधिक समय नहीं हुआ है जब हमने अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले जनलोकपाल आंदोलन को सिविल सोसाइटी के भ्रष्टाचार मुक्त उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना के संघर्ष के रूप में व्याख्यायित करने की भूल की थी। जबकि वह भाजपा को सत्ता में लाने की एक प्रायोजित रणनीति थी। रूमानियत से बाहर निकल कर किसान आंदोलन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन एवं सम्यक हस्तक्षेप समय की मांग है।
(डॉ. राजू पाण्डेय गांधीवादी चिंतक और लेखक हैं।)