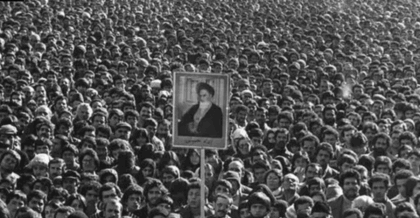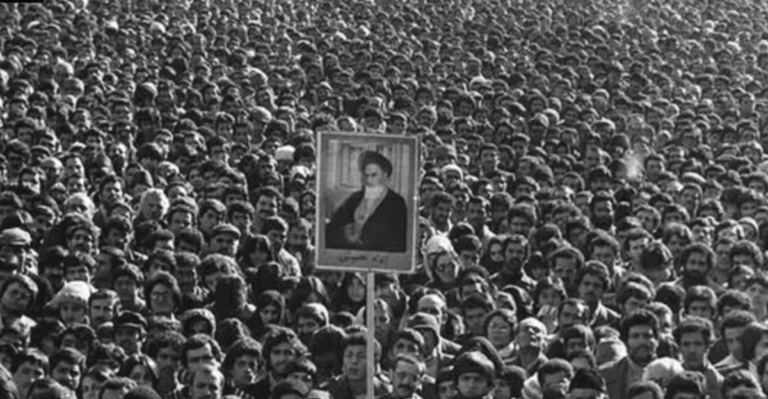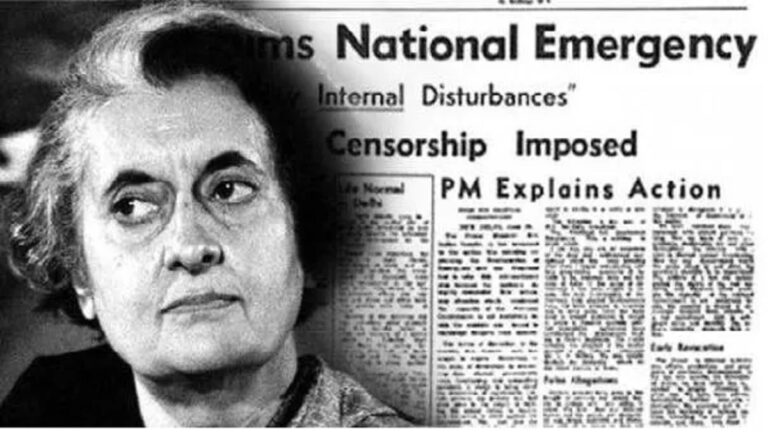वीरेन्द्र यादव की फेसबुक वॉल पर जाति और वर्ग के बारे में डा. लोहिया के विचार के एक उद्धरण* के संदर्भ में : जाति हो या वर्ग, दोनों ही सामाजिक संरचना की प्रतीकात्मक श्रेणियाँ (Symbolic categories) हैं। भले कभी इनके जन्म के पीछे समाज के ठोस आर्थिक विभाजन के कारण होते हो, जैसे जातियों के जन्म के पीछे समाज की चतुवर्णीय व्यवस्था या वर्ग विभाजन के पीछे पूँजीवादी व्यवस्था, मालिक और मज़दूर, पर जब भी किसी यथार्थ श्रेणी का प्रतीकात्मक रूपांतरण हो जाता है तब वह श्रेणी आर्थिक संरचना के यथार्थ को ज़रा सा भी व्यक्त नहीं करती है । उसके साथ आचार-विचार का एक अन्य प्रतीकात्मक जगत जुड़ जाता है । वह आर्थिक यथार्थ के बजाय अन्य प्रतीकात्मक सांस्कृतिक अर्थों को व्यक्त करने लगती है । वह एक नए मूल्यबोध का वाहक बन जाती है। जातिवादी और वर्गीय चेतना के बीच के फ़र्क़ को समझने के लिए इस बात को, वस्तु के प्रतीकात्मक रूपांतरण के साथ ही उसके मूल स्वरूप के अंत की परिघटना को समझना ज़रूरी है । यह माल के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य की तरह का विषय ही है ।
जब मार्क्सवाद में वर्गीय चेतना की बात की जाती है तो उसका तात्पर्य हमेशा एक उन्नत सर्वहारा दृष्टिकोण से होता है, उस दृष्टिकोण से जो सभ्यता के विकास में पूंजीवाद की बाधाओं को दूर करने में समर्थ दृष्टिकोण है । पर किसी भी प्रकार की जातिवादी चेतना से ऐसी कोई उन्नत विश्वदृष्टि अभिहीत नहीं होती है। डा. लोहिया के पास ऐसी किसी दार्शनिक दृष्टि का अभाव और उनके विषय को एक समाज-सुधारवादी सीमित उद्देश्य के नज़रिये से देखने का अभ्यास होने के कारण वे मार्क्सवादी वर्गीय दृष्टि के मर्म को कभी नहीं समझ पाएं और जातिवादी नज़रिये को उसके समकक्ष समझ कर जाति को भारत की विशेषता को व्यक्त करने वाली श्रेणी बताते रहे । जबकि दुनिया के इतिहास को यदि देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के शासन का हमेशा यह एक मूलभूत सिद्धांत रहा है कि समाज को चार भागों में, राजा के अलावा श्रेष्ठी या कुलीन (Patricians), सर्वसाधारण (Plebeians) और गुलाम (Slaves) में बाँट कर चलना ।
इनका भारतीय तर्जुमा क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में बिल्कुल सटीक किया जा सकता है । यूरोप में रैनेसांस के बाद पूंजीवाद के उदय से मालिक-मज़दूर के नए संबंधों के जन्म ने समाज में इस पुराने श्रेणी विभाजन को अचल कर दिया । यूरोप की तुलना में भारत में पूँजीवाद के विलंबित विकास ने पुराने जातिवादी विभाजन के अंत को भी विलंबित किया और इसमें जो एक नया और बेहद दिलचस्प पहलू यह जुड़ गया कि भारत के सामाजिक आंदोलनों की बदौलत जातिवादी विभाजन प्रतीकात्मक रूप भी लेता चला गया । इसके आर्थिक श्रेणी के बजाय अन्य प्रतीकात्मक-सांस्कृतिक अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण होते चले गए । इसमें अंग्रेज शासकों के शासन के सिद्धांतों पर रोमन साम्राज्य के शासकीय सिद्धांतों की भी एक प्रच्छन्न किंतु महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
अंबेडकर से लेकर लोहिया तक की तरह के व्यक्तित्व किसी न किसी रूप में इसी विलंबित पूंजीवाद से बने ख़ास प्रतीकात्मक जगत की निर्मिति कहे जा सकते हैं । वे जाति और वर्ग की प्रतीकात्मक धारणाओं के पीछे के ऐतिहासिक कारणों को आत्मसात् करने में विफल रहने के कारण अनायास ही वर्ग संबंधी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विरोधी हो गए और आज भी इनके अनुयायी उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं ।
* बौद्धिक वर्ग और जाति डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था —- ”
हिन्दुस्तान का बौद्धिक वर्ग, जो ज्यादातर ऊंची जाति का है। भाषा या जाति या विचार की बुनियादों के बारे में आमूल परिवर्तन करने वाली मानसिक क्रांति की सभी बातों से घबराता है। वह सामान्य तौर पर और सिद्धांत के रूप में ही जाति के विरुद्ध बोलता है।
वास्तव में, वह जाति की सैद्धांतिक निंदा में सबसे ज्यादा बढ़चढ़ कर बोलेगा पर तभी तक जब तक उसे उतना ही बढ़चढ़ कर योग्यता और समान अवसर की बात करने दी जाये। इस निर्विवाद योग्यता को बनाने में 5 हज़ार बरस लगे हैं। कम से कम कुछ दशकों तक कथित नीची जातियों को विशेष अवसर देकर समान अवसर के नए सिद्धांत द्वारा 5 हज़ार बरस की इस कारस्तानी को ख़तम करना होगा……कार्ल मार्क्स ने वर्ग को नाश करने का प्रयत्न किया। जाति में परिवर्तित हो जाने की उसकी क्षमता से वे अनभिज्ञ थे। इस मार्ग को अपनाने पर पहली बार वर्ग और जाति को एक साथ नाश करने का एक तजुर्बा होगा।”—–डॉ.राममनोहर लोहिया।
(अरुण माहेश्वरी स्तंभकार, लेखक और चिंतक है। आप आजकल कोलकाता में रहते हैं।)