पंचतंत्र में चालाक बंदर और मूर्ख मगरमच्छ की एक कहानी है, जिसमें बंदर अपना कलेजा खाने को आतुर मगरमच्छ से अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं तो अपना कलेजा नदी किनारे जामुन के पेड़ पर संभालकर रखता हूँ और वहां से लाकर ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। हमारे तमाम राज्यपालों का हाल भी पंचतंत्र की कहानी के बंदर जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह बंदर तो अपनी जान बचाने के लिए अपना कलेजा पेड़ पर रखे होने का बहाना बनाता है, लेकिन हमारे राज्यपाल सचमुच अपना विवेक दिल्ली में रखकर राज्यों के राजभवनों में रहते हैं। दिल्ली में उनके विवेक का इस्तेमाल वे लोग करते हैं जो व्यवहारिक तौर पर उनके ‘नियोक्ता’ होते हैं।
हमारे राज्यपालों की यह कहानी कोई आज-कल की नहीं, बल्कि बहुत पुरानी है, जिसे आए दिन कोई न कोई राज्यपाल देश को याद दिलाता रहता है। इस सिलसिले में राजस्थान और महाराष्ट्र के उदाहरण तो बिल्कुल ताजा हैं। पिछले तीन महीने के दौरान यह दूसरा मौका है जब किसी राज्य में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परोक्ष दखल देना पड़ा है। तीन महीने पहले जब महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की हठधर्मिता और मनमानी के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सदस्यता का मामला उलझ गया था और राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा होने के आसार पैदा हो गए थे तो प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा था।
उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बात की थी और अगले ही दिन राज्यपाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर विधान परिषद की रिक्त सीटों के चुनाव कराने के लिए कहा था और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का एलान कर दिया था। इस बार राजस्थान के मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच पैदा हुई टकराव की स्थिति भी प्रधानमंत्री के परोक्ष दखल के बाद ही खत्म हुई है और राज्यपाल ने अंतत: राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अन्यथा इससे पहले राज्यपाल तरह-तरह की दलीलें देकर सत्र बुलाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे। राज्यपाल के इस रवैये को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और फिर खुद उनसे बात की। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की बातचीत के बाद राज्यपाल के रवैये में बदलाव आया और उन्होंने सत्र बुलाना मंजूर किया।

उपरोक्त दोनों ही मामले अपने आप में अभूतपूर्व हैं, जिनमें प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा है, जबकि किसी भी दृष्टि ये मामले ऐसे नहीं थे कि प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष या परोक्ष दखल देना पडे। न तो राजस्थान के राज्यपाल के पास और न ही महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को ठुकराने का कोई संवैधानिक आधार था। न तो राजस्थान में एक सप्ताह के नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाने से कोई नई मिसाल कायम हो रही थी और न ही मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने से।
दरअसल राज्यपालों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी और मनमानी का सिलसिला करीब चार दशक पुराना है जब केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का सत्ता पर एकाधिकार टूटा और गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें भी बनने लगीं। इन चार दशकों के दौरान केंद्र में चाहे जिस दल या गठबंधन की सरकार रही हो, सभी ने अपने विरोधी दलों की राज्य सरकारों को परेशान करने और दलबदल को बढ़ावा देकर उन्हें गिराने में राज्यपालों का भरपूर इस्तेमाल किया और राज्यपाल भी खुशी-खुशी इस्तेमाल हुए या केंद्र सरकार को खुश करने के लिए अपने स्तर पर ही राज्य सरकारों को तरह-तरह से परेशान करते रहे या उन्हें अस्थिर करने का खेल खेलते रहे।
इस सिलसिले में सबसे पहले और कुख्यात उदाहरण के तौर पर जीडी (गणपतराव देवजी) तपासे का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने हरियाणा का राज्यपाल रहते हुए 1982 में लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल के पास विधायकों का बहुमत होते हुए भी अल्पमत वाली कांग्रेस के नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी और बाद में भजनलाल ने लोकदल के कुछ विधायकों से दलबदल करा कर अपना बहुमत साबित किया था। इस सिलसिले में दूसरा नाम आता है ठाकुर रामलाल का, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 1983 में तेलुगू देशम पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव को उस समय बर्खास्त कर उनके ही एक बागी मंत्री एन भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जब रामाराव अपने दिल का ऑपरेशन कराने अमेरिका गए हुए थे। ठीक इसी तरह का एक काला अध्याय 1983 में ही जगमोहन ने जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए रचा था। उन्होंने मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला को बर्खास्त कर उनके बहनोई गुल मुहम्मद शाह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी।

राज्यपालों की मनमानी के इस सिलसिले में 1989 कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई की बर्खास्तगी का मामला तो भारत के संसदीय इतिहास का एक अहम अध्याय है। बोम्मई की सरकार को तत्कालीन राज्यपाल पी वेंकट सुबैया ने मनमाने तरीके से यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है। बोम्मई ने अपनी बर्खास्तगी को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहरा दिया।
बोम्मई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार के नाम से मशहूर हुए इस मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में मील का पत्थर बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बोम्मई सरकार की बर्खास्तगी असंवैधानिक थी और उन्हें बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकार के बहुमत या अल्पमत में होने का फैसला संबंधित सदन यानी लोकसभा या विधानसभा ही हो सकता है।
इसी फैसले में शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की पुष्टि संसद के दोनों सदनों से भी होना जरुरी है और दोनों सदनों से पुष्टि हो जाने के बाद भी उस फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसी के साथ अनुच्छेद 356 लागू करने में केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए कई शर्तें भी कोर्ट ने जोड़ी थीं। यह और बात है कि सरकारों ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि राज्यपालों की कलंक-कथा में नए अध्याय जुड़ने का सिलसिला जारी रहा।

उत्तर प्रदेश में 1998 में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार थी, जिसे एक नाटकीय घटनाक्रम के बीच तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि वे महज डेढ़ दिन ही मुख्यमंत्री रह सके थे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल्याण सिंह की बर्खास्तगी को असंवैधानिक करार दे दिया था। कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। इसी तरह 1998 में बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। केंद्र में उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
राष्ट्रपति शासन का फैसला लोकसभा में पारित होने के बावजूद राज्य सभा में पारित नहीं हो सका था, लिहाजा वाजपेयी सरकार को मजबूरन राबड़ी देवी की सरकार को फिर से बहाल करना पड़ा था। इसके बाद 2005 में ऐसा ही खेल खेलते हुए झारखंड में राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने अल्पमत के नेता शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्हें महज नौ दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। बाद में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनी थी।
बिहार के राज्यपाल के रूप में ऐसी ही मनमानी सरदार बूटा सिंह ने की थी। फरवरी 2005 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, लिहाजा बूटा सिंह की सिफारिश पर मई 2005 में विधानसभा भंग कर दी गई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था।
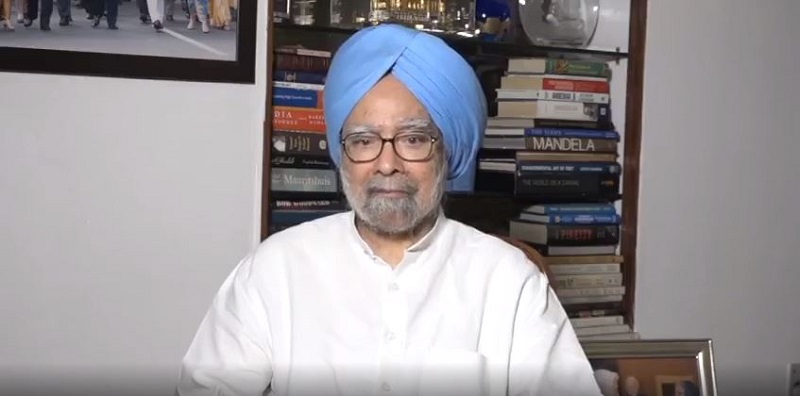
यह तो कुछ बड़े और महत्वपूर्ण उदाहरण मौजूदा सरकार के पहले के हैं, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद तो राजभवन और सत्तारूढ़ दल के दफ्तर में व्यावहारिक तौर पर कोई भेद ही नहीं रहा। पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार और राज्यपालों के लिए सरकारें बनाने-गिराने के खेल में संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक परंपराओं की बेरहमी से धज्जियां बिखेरी गई हैं। हालांकि इस दौरान दो मामलों में केंद्र सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उसने कोई सबक नहीं लिया, लिहाजा राज्यपालों के रवैये में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया।
केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद किसी राज्य सरकार को दलबदल के जरिए अस्थिर करने और फिर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शुरुआत दिसंबर 2014 में अरुणाचल प्रदेश से हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में राज्यपाल के रवैये पर सख्त टिप्पणियां करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया।
ऐसे ही मामले में मोदी सरकार को दूसरा झटका उत्तराखंड के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट से मिला। मार्च 2016 में हरीश रावत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार उस समय अल्पमत में आ गई थी, जब कांग्रेस के नौ विधायक बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए पांच दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन उनके बहुमत का परीक्षण होने से पहले ही केंद्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी थी, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार भी कर लिया था। हरीश रावत ने राष्ट्रपति के फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को असंवैधानिक करार दिया था। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी लेकिन वहां भी उसे निराशा हाथ लगी और हरीश रावत सरकार फिर बहाल हो गई।
दो-दो बार सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी हो जाने के बावजूद ‘दिल है कि मानता नहीं’ की तर्ज पर राज्यपालों के जरिए राज्यों में येनकेन प्रकारेण अपनी सरकार बनाने और विपक्षी दलों की सरकार गिराने का खेल थमा नहीं।
गोवा विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। वहां 40 सदस्यीय विधानसभा में 17 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जबकि भाजपा को 13 सीटें हासिल हुई थीं। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने की स्थापित परंपरा को नजरअंदाज करते हुए राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने भाजपा के इस मौखिक दावे को स्वीकार कर लिया कि उसके पास बहुमत है, जिसे वह विधानसभा में साबित कर देगी। मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। बाद में भाजपा ने छोटे-छोटे स्थानीय दलों के विधायकों से दलबदल कराकर और उन्हें मंत्री पद देकर अपना बहुमत बना लिया।

ठीक यही कहानी मणिपुर में भी दोहराई गई थी। 2018 के नवंबर महीने में जम्मू-कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नेशनल कांफ्रेन्स और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करने की सूचना फैक्स के जरिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भेजी तो राज्यपाल ने अपने निवास पर लगी फैक्स मशीन खराब होने की हास्यास्पद दलील देते हुए महबूबा की ओर भेजी गई सूचना मिलने से इनकार कर दिया और विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दी। कर्नाटक में भी कुछ महीनों पहले जनता दल (सेक्युलर) और कांग्रेस की साझा सरकार को अपदस्थ कर भाजपा सरकार बनाने के लिए वहां के राज्यपाल वजूभाई वाला ने जिस तरह का उतावलापन दिखाया, वह किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जनता दल (एस) तथा कांग्रेस के दल बदलू विधायकों को दलबदल निरोधक कानून से बचाने के लिए विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में भी अनावश्यक दखलंदाजी की।
कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि राज्यपाल पद के अवमूल्यन में कांग्रेस शासन के दौरान जो कमी रह गई थी, वह पिछले पांच वर्षों के दौरान तमाम राज्यपालों ने पूरी कर दी है। राज्यपालों के अमर्यादित, असंवैधानिक और गरिमाहीन आचरण के जो रिकॉर्ड इन पांच वर्षों के दौरान बने हैं, उनको अब शायद ही कोई तोड़ पाएगा।
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)













