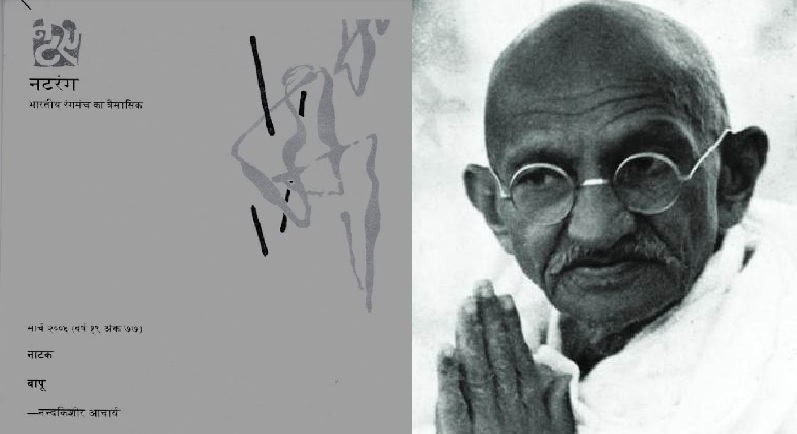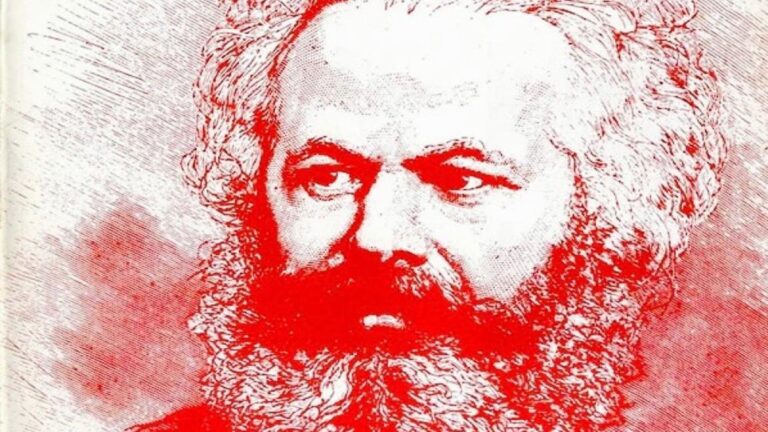नटरंग पत्रिका के मार्च 2006 के अंक में प्रकाशित नंदकिशोर आचार्य जी के ‘बापू’ नाटक को पढ़ कर कोई यदि उस पर आरएसएस की सांप्रदायिक और कपटपूर्ण विचारधारा की लेश मात्र छाया भी देखता है तो वह सचमुच तरस खाने के योग्य ही कहलायेगा। ऐसी विमर्श-विरोधी जड़ता, जो सामान्यत: धार्मिक कट्टरता के अंधेरे कुएं से पैदा हुआ करती है, विचारवान बौद्धिकों में कैसे घर कर लिया करती है, उन्हें शुद्ध फतवेबाजों के स्तर पर उतार देती है, यह सचमुच अलग से विचार का एक बड़ा विषय है । विचारधारा द्वंद्वात्मक विकास की अपनी गति को गंवा कर चेतना के कैसे संकीर्ण और सख्त ढांचों को तैयार करती है, यह उसी का एक उदाहरण है ।
बहरहाल, आचार्य जी के इस नाटक पर चर्चा को हम इसीलिये इस प्रकार की कोरी फतवेबाजी की चुनौती के दायरे से अलग रख कर अपने विचार का विषय बनाना उचित समझते हैं क्योंकि विचार-विश्लेषण के लिये अपनाए जाने वाले लक्ष्य भी विश्लेषण को प्रभावित करते हैं, विषय के प्रति न्याय में बाधा तैयार करते हैं ।
‘बापू’ नाटक गांधी जी के अंतिम दिनों के अन्तरद्वंद्वों की एक कल्पना पर रचा गया ऐसा नाटक है जो किसी भी विचारधारात्मक आदर्श के क्रियान्वयन में उसके ठोस सामाजिक रूपों की सीमाओं से पैदा होने वाली चुनौतियों की अनिवार्यता की पृष्ठभूमि में गांधी जी की मनोदशा का एक चित्र खींचता है । जैसे किसी वृहत्तर आदर्श के किसी सीमित ठोस स्वरूप की अपनी विडंबनाएं होती है, वहीं इस विडंबना की किसी भी कथा की भी अपनी विडंबनाएं हुआ करती हैं, क्योंकि वह भी हर स्थिति में जीवन के यथार्थ के विशाल फैलाव से काट कर निकाले गये एक अत्यंत छुद्र अंश को ही लेकर चलती है । इस अंश की बायोप्सी से रोग और उसके फैलाव को पकड़ने का पहलू लेखक की अपनी दृष्टि की सामर्थ्य पर ही निर्भर करता है ।
इस नाटक के पूरे ढांचे में गांधी अपने ही कांग्रेस-परिवार में कटे हुए होने की अनुभूति के साथ स्वयं से, अर्थात् अपने खुद के आदर्श अहम् से संवाद करते हुए क्रमशः परिवार के उन अन्य सदस्यों के अवस्थान को टटोल रहे हैं ,जो सभी उनकी अपनी अपेक्षाओं के बिंदु हैं, अर्थात् ऐसे बिंदु है जहां से वे अपने अहम् के सच को टटोलते रहे हैं । आजादी और देश के बटवारे के वक्त गांधी में एक पीड़ा का बोध है जिसे वे संभव है कि अपने परिजनों के दिये हुए घावों की पीड़ा की तरह ही देखते है, लेकिन दुश्मनों के वार की तरह कत्त्ई नहीं । वे उनके बिछाए कील-कांटों से जख्मी है, लेकिन पीठ पर मारे गये छुरे से नहीं !
गांधी जी का आत्म-संघर्ष और आत्म-संताप भी इसमें साफ है जब वे कहते हैं — “कोई गंभीर पाप रह गया होगा मेरी आत्मा में — उसी से बह रहा होगा ये खून ।” यह कमोबेस एक प्रकार की ऐसी बदहवासी की दशा भी हो सकती है जिसमें आदमी की नजरों से एक बार के लिये दुनिया लुप्त हो जाती है, पूरा घटना-विकास गायब हो जाता है और वह अपने तथा अन्यों के बीच के भेद पर बिल्कुल कुछ बुनियादी प्रकार के सवाल खड़े करने लगता है । जिन भेद के प्रति आदमी अपने दैनन्दिन संबंधों में पूरी तरह से बेफिक्र रहता है, वे ही तब बड़े हो कर दिखाई देने लगते हैं । दरअसल इसे ही कला कृतियों का सत्य कहा जाता हैं — अनुभूतियों के कुछ खास तीव्र क्षणों में व्यक्त हुआ सत्य ।
यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के जश्न में भाग नहीं लिया था। वे देश में जगह-जगह लगे हुए दंगों की आग को बुझाने में लगे हुए थे। लेकिन आज तक शायद ही किसी ने यह कहा होगा कि भारत की स्वतंत्रता गांधी जी की कामना नहीं थी । जब वे स्वतंत्रता के जश्न में शामिल होने से इंकार करते हैं तो कोई इतिहास के तथ्यों की समग्रता से इंकार करते हुए कह ही सकता है कि इस स्वतंत्रता से उनका कोई सरोकार नहीं था ! लेकिन यह भी एक तथ्य है कि आजादी के बाद ही गांधी जी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये एक दूसरा ही, हिंदू-मुस्लिम एकता के जरिये भारत और पाकिस्तान में मेल बैठाने का सपना देखने लगते हैं ।
दरअसल, सपने किस व्यक्ति की कामनाओं की पूर्ति करते हैं, सिगमंड फ्रायड ने इसका एक बहुत सटीक उत्तर दिया था कि सबसे पहले तो उसकी जिसकी कुछ कामनाएँ हुआ करती है, लेकिन वह अपनी कुछ कामनाओं से इंकार करता हुआ ऐसा व्यवहार किया करता है जैसे वह एक नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग व्यक्ति हो । ऐसे विभाजित व्यक्तित्व का एक रूप नहीं होता, वह अलग-अलग समय में अलग-अलग होता है । उनके हर व्यवहार में संगति हो, जरूरी नहीं होता । गांधी जी भी इसे समझते थे, वे अपने को कभी-कभी डिक्टेटर कहने के बावजूद मूलतः सामूहिक विचार-विमर्श के बीच जीने वाले व्यक्ति थे । इसीलिये कभी अपने को अन्यों पर आरोपित करते थे तो अक्सर अन्य की बातों को भी समान तरजीह दिया करते थे । कांग्रेस के नेतृत्व के साथ उनके व्यवहार में यह बार-बार प्रकट हुआ है । आजादी की लड़ाई की उनकी ‘संघर्ष, समझौता और फिर संघर्ष’ की पूरी कार्यपद्धति भी उनके व्यक्तित्व के इसी पहलू को प्रतिबिंबित करती है ।
कहना न होगा, व्यक्तित्व का ऐसा विभाजन ही अक्सर व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का कारण भी बनता है । गांधी जी अपने जीवन को ही अपना संदेश कहते हैं । हिंसा, झूठ और नाना प्रकार के छद्म की प्रवृत्तियों से भरी दुनिया में वे अहिंसा और सत्याग्रह की प्रतिमूर्ति बनना चाहते थे। यह एक अपने प्रकार का जुनून भी था । ऐसे जुनून के साथ जीने वाले व्यक्ति के सामने प्रति पल यह सवाल पैदा होना कि वह जीवित है या मर चुका है, सबसे स्वाभाविक सवाल है । यही जुनूनी विक्षिप्तता का भी कारण बनता है जब वह अपने ही रचे संसार की सबसे प्रिय चीजों से भी पूरी तरह विरत रह कर अपने आदर्श के मूर्त होने की प्रतीक्षा में जीवन बिता देता है । कई खास मौकों पर वह निश्चेष्ट हो कर अन्य से अपने अभिष्ट काम को करने की अपेक्षाएं भी करता है ।
नंदकिशोर जी के नाटक में बार-बार गांधी स्थितप्रज्ञ होने की अपनी कामना को जाहिर करते है । और बार-बार पुनः अपनी अलग भूमिका के लिये मैदान में भी उतर पड़ते हैं ।
जैसा कि हमने शुरू में ही लक्ष्य किया है, इस पूरे नाटक में गांधी अकेले स्वयं से, अर्थात् अपने अहम् से बात कर रहे हैं । उन्होंने अपने खुद के लिये जीवन के जिन लक्ष्यों को तय किया उनकी सफलता-विफलता पर स्वयं से विमर्श कर रहे हैं । और इसी क्रम में उन बिंदुओं तक पहुंचते हैं जो उनकी अपेक्षाओं के बिंदु हैं, उनके आंदोलन के तमाम सहयोगी हैं । वे उनकी नजरों में अपनी कल्पित छवि के आधार पर उन्हें समझने की भी कोशिश कर रहे हैं ।
इसीलिये इसमें नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, राजेन्द्र प्रसाद आदि सब गांधी से अलग नहीं, बल्कि उनके अपने अहम् के संघटक तत्वों की तरह ही आते हैं, जैसा कि वे वास्तविकता में भी थे । इतिहास के कुछ खास क्षणों, जैसे कैबिनेट मिशन के बारे में इन सबकी समझ का इस नाटक में कोई ऐतिहासिक मूल्यांकन नहीं किया गया है ; अर्थात् वह नाटक का विषय नहीं है । इसमें इसके सभी पक्षों के ठोस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की जांच नहीं की गई है । बल्कि यह सब तत्कालीन भारतीय राजनीति के रंगमंच पर खेले जा रहे नाटक का एक ऐसा सत्य है, जो इसके सभी चरित्रों की जद के बाहर होता है । उस सच का एक मूर्त रूप है माउंटबेटन । गांधी अफसोस करते हैं कि सब उस माउंटबेटन की बात को मान ले रहे हैं ! लेकिन वह माउंटबेटन ही तो उस नाटक के चरित्रों का बाहरी सत्य है, ब्रिटिश राज का सच है, जिसके अधिकार की जमीन पर वह पूरा संघर्ष किया जा रहा है । गांधी अफसोस करते हैं, लेकिन वे जानते हैं सब उनके परमात्मा का खेल हैं । “मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी योजनाओं की सफलता उस पर नहीं, बल्कि हम सबके भाग्य के सर्वोपरि निर्णायक ईश्वर पर निर्भर होती है ।”
इस नाटक में अपने ही लोगों के दिये गये घावों के संदर्भ में इतिहास के तथ्य के रूप में खास तौर पर कैबिनेट मिशन और उसके बारे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों के फैसले की चर्चा की गई है जिसके बारे में बताया गया है कि गांधी जी उनसे जरा भी सहमत नहीं थे । यद्यपि इस बात में कितना तथ्य है और कितना नहीं, यह इस नाटक का विषय नहीं है । फिर भी यह एक सवाल रह जाता है कि कैबिनेट मिशन के बारे में ही गांधी के साथ कांग्रेस के बाकी नेतृत्व का ऐसा कैसा मतभेद था जिसने गांधी जी को इस हद तक ‘मर्माहत’ कर दिया था !
डी जी तेंदुलकर की किताब ‘Mahatma : The life of Mohandas Karamchand Gandhi’ के सातवें खंड में इस पर पूरे विस्तार से चर्चा है । 6-7 जुलाई 1946 के दिन इस विषय पर निर्णय के लिये मुंबई की भंगी कॉलोनी में कांग्रेस वर्किंग की बैठक के बाद एआईसीसी की बैठक हुई थी । तेंदुलकर लिखते हैं —
“कार्रवाई को शुरू करते हुए मौलाना आजाद ने पिछले छः सालों में, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, देश के घटना-चक्र की एक समीक्षा पेश की । उनकी राय में भारत के इतिहास में ये छः साल अत्यंत महत्वपूर्ण थे और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तथा भारत के अपने स्वतंत्रता संघर्ष में हुए दूरगामी परिवर्तनों की ओर उन्होंने संकेत किया । देश आजादी के मुहाने पर था । इस लक्ष्य को पाने के लिये अब सिर्फ एक और कदम बाकी रह गया था ।
“नेहरू ने अध्यक्ष पद ग्रहण करते हुए कहा कि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि प्रस्तावित संविधान सभा की योग्यता, अयोग्यता के आधार पर किसी प्रस्ताव को स्वीकारा या अस्वीकारा जाए । वह एक महत्वपूर्ण सवाल है, देश की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ सवाल । …
आजाद ने इसके बाद ही वर्किंग कमेटी का 26 जून का प्रस्ताव पेश किया । …समाजवादियों ने प्रस्ताव का विरोध किया और गांधी जी की प्रार्थना सभाओं के भाषणों को उद्धृत किया । इस प्रस्ताव के पक्ष में 7 जुलाई को एआईसीसी को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था —
“मैंने अक्सर कहा है कि मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी योजनाओं की सफलता उस पर नहीं, बल्कि हम सबके भाग्य के सर्वोपरि निर्णायक ईश्वर पर निर्भर होती है । आपकी तरह मैं यहां अधिकारपूर्वक नहीं आया हूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि मुझे बर्दाश्त किया जाता है । मुझे बताया गया है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में मेरी पहले की कुछ उक्तियों से जन-मानस में बहुत उलझन पैदा हो गई है । सत्याग्रही के नाते मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता हूं कि सम्पूर्ण सत्य और केवल सत्य ही बोलूँ । मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता । मानसिक दुराव से मुझे चिढ़ है । लेकिन भाषा अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का एक अपूर्ण माध्यम ही है । कोई भी व्यक्ति अपनी भावना या विचार को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता । प्राचीन काल के ऋषियों और पैगंबरों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा था ।
“कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के विषय में मैंने जो कहा माना जाता है उसके सम्बन्ध में अखबारों में क्या प्रकाशित हुआ है यह मैंने नहीं देखा है । मैं सभी अखबार खुद नहीं पढ़ सकता । मेरे सहयोगी और सहायक जो कुछ मेरे सामने रख देते हैं उसी पर निगाह डाल कर मैं संतोष मान लेता हूँ । मैं मानता हूँ कि ऐसा करने से मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है । अखबारों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उससे कुछ ऐसा भ्रम पैदा हो गया लगता है कि मैंने दिल्ली में एक बात कही और अब कुछ और कह रहा हूँ । दिल्ली के अपने एक भाषण में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के बारे में मैंने यह अवश्य कहा था कि जहां पहले मुझे प्रकाश दिखाई देता था, वहां अब अंधकार दिखाई देता है । अब भी वह अंधकार छँटा नहीं है । शायद और भी घनीभूत हो गया है ।
अगर मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई देता तो मैं कार्यसमिति से संविधान-सभा-विषयक प्रस्तावों को अस्वीकार करने को कह सकता था । कार्य-समिति के सदस्यों के साथ मेरे संबंधों को आप जानते हैं । बाबू राजेन्द्र प्रसाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने चम्पारन में मेरा दुभाषिया और मुन्शी बनना पसन्द किया । फिर हैं सरदार ! उन्हें मेरी जी-हजूरी करने वाला कहा जाता है । उन्हें यह बुरा नहीं लगता । बल्कि वे इसे एक प्रशस्ति मान कर उछालते फिरते हैं । वे संघर्ष के अग्रदूत हैं । कभी वे पाश्चात्य ढंग की पोशाक पहनते थे और उसी ढंग से खाते-पीते थे ।
जबसे उन्होंने मुझसे नाता जोड़ा है, मेरा कहा उनके लिए ब्रह्मवाक्य बन गया है । लेकिन इस मामले में वे मुझसे सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि पहले मौकों पर जब आपकी सहज बुद्धि कुछ बात कहती थी तो आप उसका दलील से समर्थन करके हमारे दिल और दिमाग दोनों को संतुष्ट कर दिया करते थे, लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं । उत्तर में मैंने उनसे कहा कि मेरा हृदय तो आशंकाओं से भरा हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं कोई कारण नहीं ढूँढ पा रहा, अन्यथा मैं आपसे इन प्रस्तावों को बिल्कुल ठुकरा देने को ही कहता ।… लम्बे विचार-विमर्श के बाद वे लगभग सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँचे हैं वह आपके सामने है । कार्य-समिति के सदस्य आपके विश्वस्त और परखे हुए सेवक हैं । …आप सब तपे-परखे और पुराने योद्धा हैं । सिपाही खतरे से नहीं डरता । वह तो खतरे को देख कर उमंग से भर जाता है । अगर प्रस्तावित संविधान-सभा में दोष है तो उन्हें दूर करना आपका काम है । वह आपके लिए संघर्ष की चुनौती होनी चाहिए, अस्वीकार करने का कारण नहीं ।”(पृष्ठ — 145-146)
कैबिनेट मिशन और उस पर गांधी जी के मन-मस्तिष्क की ऊहापोह और कांग्रेस की कार्य-समिति के प्रति उनके विश्वास को बताने वाले इतने बड़े उद्धरण को यहां देने का उद्देश्य अलग से बताने की जरूरत नहीं है । गांधी जी के मन में सवाल थे, लेकिन अपने ही लोगों ने उन्हें जख्म दिये, मौलाना आजाद ने सच को छिपाया आदि की तरह के खुद के ठगे जाने का भाव, लेखक की कल्पना की पैदाईश हो सकते हैं, तथ्य इसकी ओर कोई साफ संकेत नहीं देते । गांधी जी ने अपने इस भाषण में भाषा की सीमा के बारे में बहुत सही संकेत दिया था । किसी भी लेखक के लिये यह जरूरी होता है कि वह चरित्र को उसकी भाषा की सीमा के परे जाकर पेश करे । और जाहिर हैं कि ऐसा करते हुए ही लेखक के अपने सोच का परिप्रेक्ष्य सहज ही चरित्र के चित्रण में भी प्रवेश कर जाता है । विश्लेषण विश्लेषक के सोच से अलग नहीं हो पाता है ।
बहरहाल, आचार्य जी के इस नाटक को पढ़ कर हमें अनायास ही आज के समय के प्रसिद्ध मार्क्सवादी फ्रांसीसी दार्शनिक ऐलेन बदउ के नाटक L’Incident d’Antioche (एंटियोक की घटना) की याद आती है । अपने ब्लाग की टिप्पणियों के संकलन के पहले खंड की भूमिका, ‘विमर्श ही नाउम्मीदी का साहस, भैरव भाव है’ में हमने उस नाटक पर काफी विस्तार से चर्चा की थी और उसी प्रसंग में वहां गांधी जी के अंतिम दिनों के आत्म-संघर्ष का पहलू भी आ गया था ।
बाद्यू के उस नाटक की पृष्ठभूमि में ईसाई मिशन में लगे सेंट पॉल्स और पीटर के बीच एंटियोक में बाइबल की सार्वलौकिकता के विषय पर हुआ संघर्ष है । नाटक का मूल विषय यह है कि क्या किसी भी क्रांतिकारी को परंपरागत रूढ़ियों का पालन करते रहना चाहिए ? मसलन्, देवदूत पीटर को क्या पुराने यहूदी रीति-रिवाजों का पालन जारी रखना चाहिए ; मसलन्, आज क्रांति-विमुख लोगों को बाजार अर्थ-व्यवस्था और संसदीय जनतंत्र की निर्विकल्पता से ही चिपके रहना चाहिए ? अथवा ईसाइयों ने यहूदी-विद्वेष का जो रास्ता अपनाया, या पौल पौट के खमेर रूज ने पुराने काल के समर्थकों के सफाये की जो नीति अपनाई, उस लाइन को अपनाया जाना चाहिए ? इस नाटक के एक अंश में क्रांति का नेता कमिउ क्रांति हो जाने के बाद कहता है — मेरा काम पूरा हो गया, अब चलता हूं ।
उसका साथी डेविड उससे कहता है कि आज जब काम करने का समय आया है, तभी तुम मुंह फेर रहे हो । तो कमिउ कहता है — “विजय के बाद जो बचता है वह है पराजय ।… फौरन पराजय नहीं, जो भी वर्तमान के साथ निबाह करके चलेगा उसकी धीरे-धीरे निश्चित पराजय ।…उस प्रकार की पराजय की शान को मैं तुम्हारे लिये छोड़ता हूं, किसी अहंकारवश या धीरज की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिये क्योंकि मैं उसके लिये उपयुक्त नहीं हूं ।”
बाद्यू इसकी व्याख्या करते हुए एक जगह लिखते हैं कि उसने इसलिये नई सत्ता का त्याग किया क्योंकि कुछ लोग सिर्फ विध्वंस से प्यार करते हैं और चूंकि वह देख रहा है कि अब एक नये राज्य के पुनर्निर्माण का काम होगा, उस पुनर्निर्माण में उसे एक प्रकार के दोहराव की ऊब दिखाई देने लगती है, इसीलिये उसकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है । (Alain Badiou, The Communist Hypothesis, Verso, 2015, page – 15-17)
क्रांति का नेता कमिउ तैयार नहीं था पुनर्निर्माण की एक धीमी और निरंतर जारी उबाऊ प्रक्रिया के बीच से आने वाली अनिवार्य विफलता को अपनाने के लिये । लेकिन क्रांति की इस तात्विक सीमा के साथ ही, इस नाटक में उसकी विफलता का आगे एक और, दूसरा आख्यान भी आता है, जब क्रांति के बाद के नये शासक डेविड की मां पौला उससे कहती है — ‘तुम सत्ता छोड़ दो ।’
डेविड मां से कहता है कि ‘तुम मेरी मां होकर प्रति-क्रांतिकारी काम क्यों कर रही हो’,
तो पौला उसे कहती है — “प्रति-क्रांति तुम हो । तुमने न्याय के सारे बोध को गंवा दिया है । तुम्हारी राजनीति कुत्सित है ।…सुनो । …हमारी परिकल्पना, सिद्धांततः, यह नहीं थी कि हम एक अच्छी सरकार की समस्याओँ का समाधान करेंगे ।…हमने कहा था कि दुनिया एक ऐसी नीति के रास्ते पर चल सकती है जिसे बदला जा सकता है, राजनीति को ही खत्म कर देने वाली नीति । …उस परिकल्पना के ऐतिहासिक स्वरूप को राजसत्ता ने निगल लिया है । एक मुक्तिदायी संगठन का राजसत्ता में विलय हो गया है । …कोई भी सही नीति यह दावा नहीं कर सकती है कि वह अब तक किये जा चुके कामों की ही निरंतरता है । हमारा उद्देश्य एक बार और हमेशा के लिये उस चेतना को मुक्त कर देने का है जो न्याय, समानता को कायम करती है और राजसत्ता और दरबारों की साजिशों का हमेशा के लिये अंत करती है, और उस बची हुई जमीन का भी सफाया करती है जिससे पैदा होने वाली सत्ता की लिप्सा आदमी ऊर्जा के प्रत्येक रूप को लील लेती है ।“
…डेविड मां से कहता है — “दुनिया हमेशा के लिये बदल गई है । विश्वास करो । मेरी प्यारी मां तुम चीजों को नीचे से देख रही हो । तुम निर्णय लेने वालों में नहीं हो ।“
“पौला — यही पुरानी आजमाई हुई चाल है ।… जरूर तुम कुछ नया करोगे । तुम सूरज को भूरे रंग से रंग दोगे ।“
इसी सिलसिले में बौखला कर डेविड मां से पूछता है — कहो तो, तुम कौन हो ? …तुम निश्चय ही हमें और शक्तिशाली बनने के लिये नहीं कह रही हो । बल्कि हमें सत्ता को त्याग देने, आने वाले लंबे काल के लिये उसे छोड़ देने के लिये कह रही हो ।
तो पौला कहती है, “मानव जाति की महानता सत्ता में नहीं है । बिना परों वाले दोपाये का खुद पर नियंत्रण हो, और वह, जो उतना संभव भी नहीं लगता, प्रकृति के सभी नियमों, इतिहास के सभी नियमों के खिलाफ जाए और उस राह पर चले जिसमें हर व्यक्ति प्रत्येक के प्रति समान होगा । सिर्फ कानून में नहीं, भौतिक यथार्थ में भी।“ (जोर हमारा)
इसपर डेविड कहता है, “ तुम इतनी पागल हो !“
पौला कहती है — “नहीं, मैं नहीं । मैं तुमसे कहूंगी सारे उन्माद को छोड़ो । तुम्हें बहुत धीर-स्थिर हो कर निर्णय करना है । जो भी व्यक्ति मरीचिका के पीछे भागता है, वह यह नहीं समझ सकता है । विजय और समग्रता के प्रति अपने आग्रह को भूल जाओ । वैविध्य के सूत्र को पकड़ कर चलो ।“
…“राजनीति का अर्थ एक राजनीतिक भविष्य दृष्टि के आधार पर इकट्ठा होना है ताकि आदमी राजसत्ता की मानसिक जकड़बंदी से मुक्त रह सके ।“ (वही, पृष्ठ – 15-22) (जोर हमारा)
बाद्यू के नाटक के इस पूरे प्रसंग का आचार्य जी के ‘बापू’ नाटक के संदर्भ में स्मरण शायद ही किसी को अप्रासंगिक लगेगा । आजादी की लड़ाई के दौर में हमेशा नेतृत्व की कमान थामे रहने वाला, खुद को डिक्टेटर तक कहने वाला नायक आजादी के ठीक बाद अपने को अकेला और नई राजसत्ता के खेलों में पूरी तरह से अनुपयुक्त पाता है, उनसे विरत हो जाता है । वह अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने आया था, उसे तोड़ दिया । अब आजाद भारत का नया राज्य बनेगा, नई जंजीरें तैयार होगी ।
सवाल है कि बापू उसमें क्यों शामिल होंगे ! कमिउ की तरह क्या वे नहीं देख रहे थे कि जीत के बाद आगे सिर्फ हार खड़ी प्रतीक्षा कर रही है — फौरन नहीं, धीरे-धीरे । इस पराजय को सबको मानना होगा क्योंकि यह निर्रथक पराजय नहीं होगी, एक प्रकार के स्वातंत्र्य से स्फूरित पराजय, जीवन में किंचित शांति लाने और राज्य को मजबूत करने वाली पराजय । गांधी इस पराजय के गौरव को दूसरों के लिये छोड़ने को तैयार थे, क्योंकि नाफरमानी के उनके विचार क्यों किसी के भी फरमान को मानने के लिये मजबूर होंगे ! वे आजादी की लड़ाई के उत्साह की समाप्ति के बाद की लोगों की तिरछी नजरों की कल्पना कर पा रहे थे और अपने को उन बुरी नजरों के वृत्त के बाहर रखना ही श्रेयस्कर समझते थे ।
उन्होंने अपने जीवन को ही अपना संदेश कह कर राजनीति मात्र को उस भविष्य दृष्टि का रूप देने की बात कही थी जो नैतिक स्वातंत्र्य के बल पर आदमी को राजसत्ता के मानसिक दबावों से मुक्त रहने की ताकत देती है, नाफरमानी की ताकत देती है, जैसा कि बाद्यू के नाटक में डेविड की मां पौला डेविड से कहती है । रूस में क्रांति के पहले लेनिन ने एक बार चिंतित हो कर त्रातस्की से पूछा था कि यदि क्रांति विफल हो जाती है तो क्या होगा, तो त्रातस्की का जवाब था, यदि क्रांति सफल हो जाती है तो क्या होगा ?
‘बापू’ नाटक में क्रांति और सत्ता विमर्श की इसी कहानी को गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, राजेन्द्र प्रसाद और सुभाष बाबू के बीच बंटवारे और हिंदू-मुस्लिम तनाव आदि के प्रसंगों में अपने प्रकार से पेश किया गया है । क्रांति और उसके बाद क्या ? — यह सामाजिक परिवर्तन के हर ऐतिहासिक संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ एक चिरंतन प्रश्न है । किसी भी ठोस सत्ता विमर्श का त्रिक इसमें एक नये राज्य के निर्माण की समस्याओं के योग से ही तैयार होता है । राजसत्ता-केंद्रित परिवर्तन का सबसे त्रासद पहलू वह होता है जब जनरोष आदमी के सामयिक क्रोध की तरह भड़कता है, लेकिन किसी विवेकपूर्ण परिणति तक जाने के बजाय कुछ मायनों में और भी पतन की दिशा में बढ़ जाता है ! गांधी भी इसे जानते थे । इसीलिये वे कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित संविधान-सभा को पूरी तरह से ठुकराने के बजाय आजमाने पर बल देते हैं । इधर के सालों में, अफ्रीका और मध्य एशिया के अरब वसंत (2010-2014) के तूफानी घटना क्रम को देख लीजिए अथवा सारी दुनिया में दक्षिणपंथ के नये उभार को, इस त्रासदी को समझना आसान हो जायेगा ।
‘बापू’ नाटक में कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बीच मतभेद की तरह के कथित ऐतिहासिक तथ्यों का इसलिये कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इस नाटक का उद्देश्य ही इतिहास का कोई नया प्रामाणिक आख्यान पेश करना नहीं है । यह सत्य, अहिंसा और राजसत्ता के लिये संघर्ष के विषय पर एक निरंतर विमर्श की प्रस्तावना है । यह विमर्श ही इन सभी विषयों पर आदमी के अंतर के शून्य को भरने का और मानव-कल्याण के समताकारी व्योम से उसके लय का, संगति बनाये रखने का अकेला साधन है ।
इसी मायने में यह नाटक हमारे समय का एक महत्वपूर्ण नाटक है ।
(अरुण माहेश्वरी वरिष्ठ लेखक और स्तंभकार हैं आप आजकल कोलकाता में रहते हैं।)