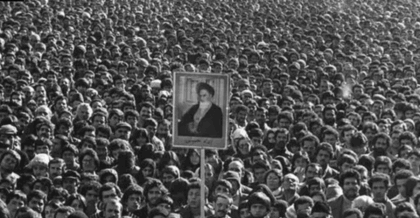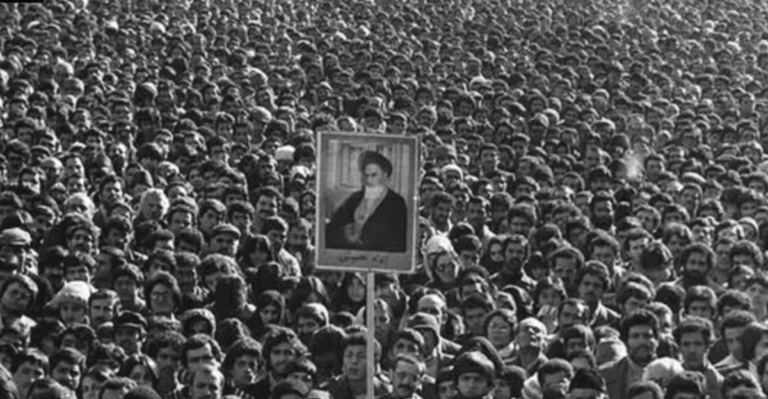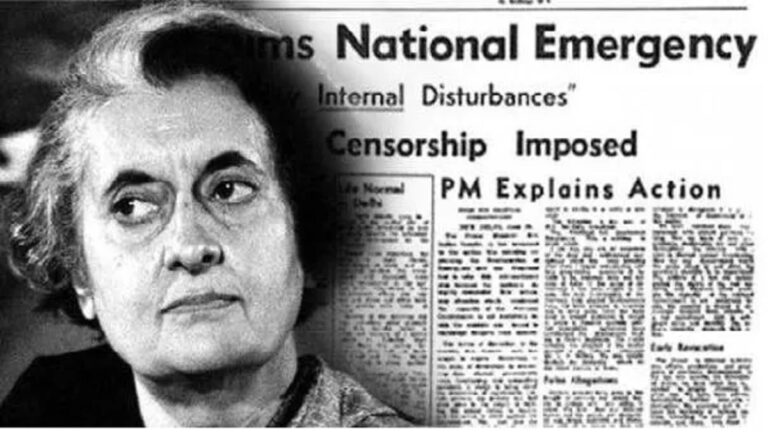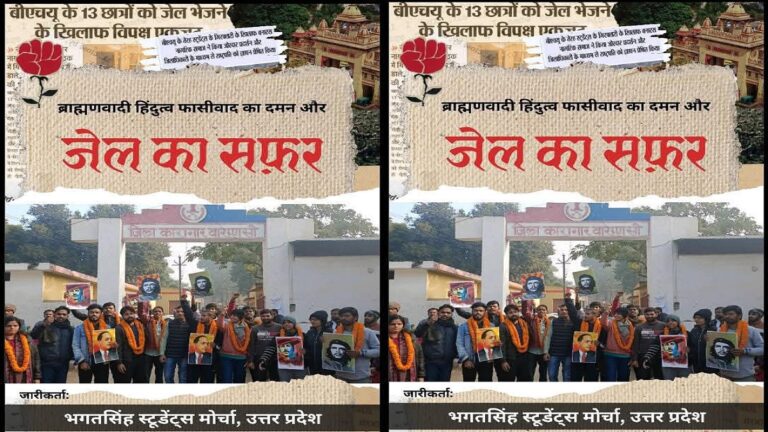हरी सैन्य वर्दी में जमीन पर सूखे पत्तों के बीच मृत एक बुजुर्ग, जिनकी खुली आँखें जंगल को अब भी निहार रही हैं, की तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, इस खबर के साथ कि सीपीआई माओवादी के महासचिव कॉमरेड वासवराज मुठभेड़ में मारे गए। निश्चित ही यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर है।
सीपीआई माओवादी से कोई सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन इस पर कोई दो- राय नहीं हो सकती कि इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता लड़ते हुए उस जंगल के अंदर ही मारे जा रहे हैं, जिसे बचाने का दावा वो करते हैं। माओवादी नेतृत्व के जो लोग मुठभेड़ में नहीं मारे गए वो फर्जी मुठभेड़ में पकड़कर मार दिए गए। जो इन दोनों तरीकों से नहीं मारे गए, वे आदिवासियों के बीच जंगल में रहते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से मारे गए। अपने उद्देश्य के लिए यह समर्पण कहीं और देखने को नहीं मिलता।
इस मौत पर लिखते हुए मुझे याद आ रहा है कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो एटीएस के एक अधिकारी ने मुझसे पूछा था, आप मानवाधिकार वाले तभी क्यों बोलते हैं जब हम उन्हें मारते हैं, जब वो मारते हैं, तब आप लोग चुप रहते हैं। उस समय मैंने उनका जो भी जवाब दिया था, लेकिन अब इसका एक और स्पष्ट जवाब है मेरे पास। ऐसे समय में जबकि माओवादी हथियार रखकर शांतिवार्ता की अपील कर रहे हैं, इस तरह की हत्या क्यों की गई कि जो माओवादियों को आगे की हिंसा के लिए प्रेरित करे?
इस साल जनवरी से हो रही आदिवासियों/माओवादियों की हत्याएं इसका प्रमाण हैं कि सरकार की मंशा माओवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि लोगों पर “स्टेट पावर” का प्रदर्शन करना है।
पिछले दो महीने से माओवादी हथियार रखकर सरकार से शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, ढेरों मानवाधिकार संगठन और बुद्धिजीवी व्यक्ति शांतिवार्ता में जाने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। ऐसे समय में भी उनसे बातचीत न करके उन्हें मारते जाना गैर न्यायिक हत्या और मानवाधिकार का उल्लंघन ही माना जाएगा।
उनकी हत्या जो इसी देश के मेधावी नागरिक हैं, और सरकार की व्यवस्था से सहमत नहीं हैं।
वासवराज जिनके बारे में उनके जीते जी किसी ने नहीं जाना, यह भी नहीं कि वे 72 साल के थे, के बारे में खबरें आ रही हैं कि वे अपने कॉलेज के मेधावी छात्र थे, अच्छे खिलाड़ी थे और अन्याय के सख्त विरोधी थे, अपने छात्र जीवन से ही वे हर तरह के अन्याय का विरोध करते रहे।
इसके पहले एक युवा डॉक्टर रवि के मारे जाने की खबर भी आई थी, जो माओवादी दस्ते में शामिल हो गए थे। माओवादी क्या चाहते हैं और सरकार उनसे बातचीत क्यों नहीं करना चाहती, मुझे लगता है इसके कुछ ठोस कारण हैं और इस समय इस पर बात करना बेहद जरूरी है।
माओवादियों से युद्ध विराम और शांति वार्ता की एक पृष्ठभूमि से इसे आसानी से समझा जा सकता है। माओवादियों की आंध्र प्रदेश इकाई जब 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ वार्ता में आयी थी, तो उन्होंने प्रदेश के कई बड़े जमींदारों की सैकड़ों एकड़ की जमीन का विवरण सरकार के सामने प्रस्तुत करते हुए यह मांग की थी कि उन्हें भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाए।
इन बड़े जमींदारों में कई विभिन्न संसदीय पार्टियों से जुड़े लोग थे।
उन्होंने मांग की थी कि आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन पर कब्जाकर उसे नष्ट करने वाले समझौते, जो पूंजीपतियों से किए गए हैं, उन्हें रद्द कर इन संसाधनों पर आदिवासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मांगे रखी थीं, जो समाज के जनवादीकरण से जुड़ी थीं।
इस शांति वार्ता के लिए आंध्र प्रदेश माओवादी पार्टी के सचिव राम कृष्ण जब बाहर आए थे, तो वे जिस होटल में ठहराए गए थे, वहां उनसे मिलने वालों की लंबी लाइन लग गई थी। मिलने वाले ये चाहते थे कि माओवादी पार्टी उनकी जमीन फलां जमींदार से मुक्त करा दे, फलां जमींदार के उत्पीड़न से उन्हें, उनके गांव की औरतों को बचा ले या उनका फलां रुका हुआ काम जिसमें दौड़ते-दौड़ते उनकी चप्पल घिस गई, सरकार पर दबाव डलवाकर करवा दे।
पत्रकारों, हम जैसे आम लोगों के लिए यह बेहद आश्चर्यजनक बात थी और सरकार के लिए यह बेहद शर्मनाक घटना थी।
सरकार माओवादियों की मांगों पर सहमत नहीं हुई और वार्ता टूट गई।
मौजूदा सरकार भी जानती है कि वह माओवादियों की इन मांगों को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि उनकी नाभि सामंतों और पूंजीपतियों से जुड़ी है। अगर वह शांतिवार्ता में जाती है तो तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार की तरह यह सरकार भी एक्सपोज होगी। इस पृष्ठभूमि के कारण ही सरकारें चाहती नहीं कि वे शांतिवार्ता में जाएं। इसके बदले वे माओवादियों को अपराधियों की तरह मारने में अधिक यकीन करती हैं। अधिकतर फर्जी मुठभेड़ों में गैरकानूनी तरीके से और कई बार असली मुठभेड़ में भी। माओवादियों को मारने के लिए सरकार ने जो तरीका अपनाया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही फटकार के साथ रोक लगाई थी। उस समय उसका नाम सलवा जुडूम था, यानि आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करना। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद
मौजूदा सरकार ने उसी तरीके को दूसरे नामों से लागू करना शुरू किया है। वह गांवों में डीआरजी का गठन कर रही है, जिसमें आदिवासी और समर्पण कर चुके माओवादी हैं, यानि जीते या हारे कोई भी शहीद आदिवासी ही होंगे, उजड़ेगा जंगल ही।
मौजूदा सरकार के गृहमंत्री ने यह घोषणा की है कि वे सन 31 मार्च 2026 तक माओवाद का सफाया कर देंगे। उसके बाद से ही बस्तर/ छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के मारे जाने की खबर लगभग हर दिन आ रही है। इस मारकाट के बीच जब माओवादियों ने मार्च अंत में शांतिवार्ता की पेशकश की, तो सरकार और पूंजीपतियों की मीडिया ने यह प्रचारित किया, कि माओवादी कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए शांतिवार्ता की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात है कि अगर ऐसा है भी, तो इसी का फायदा उठाकर शांतिवार्ता में जाकर बिना खून खराबे के माओवादी समस्या को खत्म करने में क्या बुराई थी? क्या ये रास्ता सही रास्ता नहीं होता?
दरअसल बात ये है ही नहीं। असल बात ये है कि यह सरकार माओवादियों की मांगों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और शांतिवार्ता में जाकर माओवादियों की जनवादी, किसान समर्थक, मजदूर समर्थक, महिला समर्थक, आदिवासी समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक मांगों को सामने आने के बाद, मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद उन्हें मानने से इनकार करके खुद को एक्पोज नहीं करना चाहती। इसकी बजाय वो माओवादियों की मांगों पर खून का पोंछा मारकर उन्हें अपराधी के तौर पर दिखाते रहना चाहती है। यह सरकार की “पावर स्टेट” दिखाने की पॉलिसी है। जी हां, मानवाधिकार संगठन इसे गलत मानते हैं, और इसकी आलोचना करते हैं। “ऑपरेशन सिंदूर” के युद्धोन्मादी शक्ति प्रदर्शन के बाद माओवादियों के बड़े नेता वासव राज को मारकर वह अपनी छवि “पावर स्टेट” की ही गढ़ना चाह रहे हैं, मानवाधिकारी लोकतांत्रिक स्टेट की नहीं। इस तरीके से सरकार “माओवादियों” की हत्या कर सकती है, लेकिन “माओवाद” की नहीं। बल्कि ऐसा करके सरकार माओवाद की विचारधारा का विस्तार कर रही है, वह साबित कर रही है कि माओवादी विचारधारा राज्य की पक्षधरता के बारे में सही बोलती है। इसी कारण वासवराज की हत्या सीपीआई (माओवादी) में आखिरी कील नहीं (जैसा कि मीडिया कह रही है), बल्कि भारतीय राज्य पर एक हथौड़ा साबित हो सकती है।
शांतिवार्ता की पेशकश करने वाली पार्टी के शीर्ष की इस तरह से हत्या किए जाने पर किसी भी मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता को निंदा ज़रूर करनी ही चाहिए।
जसिंता केरकेट्टा की यह कविता इस वक्त बेहद प्रासंगिक है, इसके साथ अपनी बात समाप्त कर रही हूं।
सेना का रुख़ किधर है
…………………………
युद्ध का दौर खत्म हो गया
अब सीमा की सेना का रुख़ उधर है
मेरा स्कूल-कॉलेज, गांव-घर, जंगल-पहाड़ जिधर है
कौन साध रहा है अब
चिड़ियों की आंख पर निशाना
इस समय ख़तरनाक है सवाल करना
और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना
क्योंकि संगीनों का पहला काम है
सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना
खत्म हो रही है उनकी
बातें करने और सुनने की परंपरा
अब सेना की दक्षता का मतलब है
गांव और जंगल पर गोलियां चलाना
और सवाल पूछते विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाना
यह दूसरे तरीके का युद्ध है
जहां संभव है
गांव में बहुतों के भूखे रह जाने का
किसानों के आत्महत्या कर लेने का
और शहर में आधे लोगों का
बहुत खाते हुए, तोंद बढ़ाते हुए
अपनी देह का भार संभालने में असमर्थ
एक दिन नीचे गिर जाने का
और अपनी ही देह तले दबकर मर जाने का
किसी युद्ध में बम के फटने से
यह शहर धुंआ-धुंआ नहीं है
यह तो विकास करते हुए
मंगल ग्रह हो जाने की कहानी है
इस विकास में न बच रहे जंगल-पहाड़
न मिल रही सांस लेने को साफ़ हवा
और लोग ढूंढ रहे कि कहां साफ़ पानी है
कोई युद्ध न हो तब भी सेना तो रहेगी
आख़िर वह क्या करेगी
वह कैंपों के लिए जंगल खाली कराएगी
जानवरों की सुरक्षा के लिए
गांव को खदेड़ कर शहर ले जाएगी
और शहर में सवाल पूछते
गांव के बच्चों पर गोली चलाएगी
आख़िर क्यों सीमा की सेना का रुख़ उधर है
मेरा स्कूल-कॉलेज, गांव-घर, जंगल-पहाड़ जिधर है
(छावनियों के खिलाफ़ छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा में लड़ते लोगों को समर्पित)
जसिंता केरकेट्टा
(सीमा आजाद मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं।)