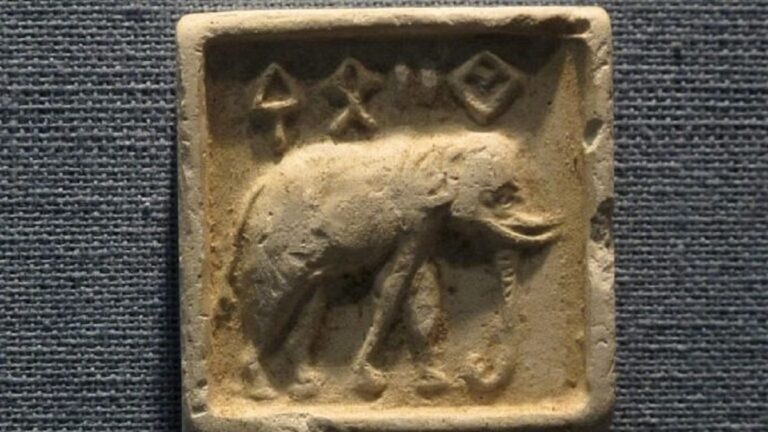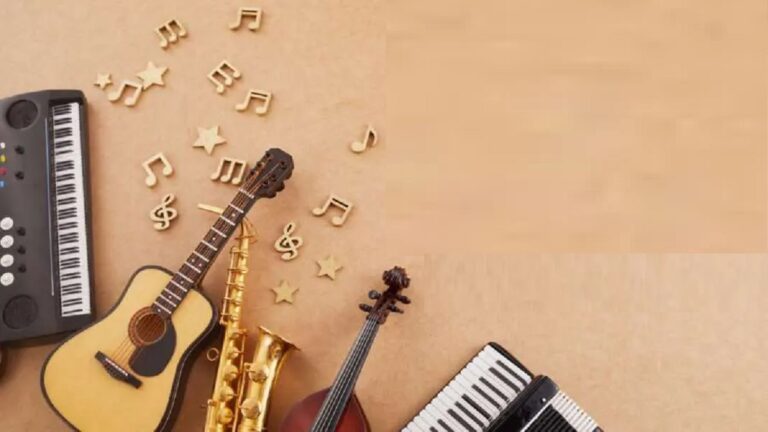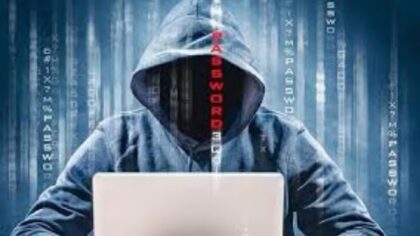राजनीतिक प्रणाली: राज्यपाल और उपराज्यपाल- महिला प्रतिनिधित्व और लैंगिक अंतर
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत में 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाता है। राज्यपाल और उपराज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब तक 24 महिलाएँ राज्यों की राज्यपाल और 5 महिलाएँ केंद्र शासित प्रदेशों की उपराज्यपाल रह चुकी हैं।
हालाँकि, आज तक दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में किसी महिला उपराज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। यह वास्तव में निराशाजनक है कि इन नियुक्तियों में भी महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई है। यही कारण है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक अंतर बना हुआ है। इस अंतर को दूर करने के लिए इन नियुक्तियों में महिलाओं को समान भागीदारी दी जानी चाहिए।
सन् 1947 से सन् 2025 तक: केवल 18 महिला मुख्यमंत्री – लैंगिक अंतर
भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था। ऐतिहासिक क्रम में, भारतीय कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती सुचेता कृपलानी (हरियाणा के अंबाला की बेटी, सन् 1963 से सन् 1967 तक) को उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय प्राप्त है। श्रीमती सुचेता कृपलानी से लेकर श्रीमती रेखा गुप्ता तक, कुल 18 महिलाएँ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन सन् 1950 से सन् 2025 तक, 350 से अधिक पुरुष मुख्यमंत्री रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से भी संबंधित रही हैं। संविधान लागू होने के बाद से सन् 2025 तक केवल 12 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में महिला मुख्यमंत्री रही हैं। वर्तमान समय (सन् 2025) में भारत के 27 राज्यों और सात केंद्र शासित क्षेत्रों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है।
अब तक केवल दो मुस्लिम महिलाएँ मुख्यमंत्री बनी हैं – सैयदा अनवरा तैमूर (असम की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री) और श्रीमती महबूबा मुफ्ती (जम्मू-कश्मीर की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री)। 18 महिला मुख्यमंत्रियों में से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पाँच-पाँच महिलाएँ विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री रही हैं, जबकि 8 महिलाएँ अन्य राजनीतिक दलों से संबंधित हैं। वर्तमान में कांग्रेस शासित राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि भाजपा नीत एनडीए की राज्य सरकारों में केवल दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता (20 फरवरी, 2025 से) मुख्यमंत्री हैं।
संक्षेप में, मार्च 2025 तक केंद्र शासित प्रदेशों सहित 30 मुख्यमंत्रियों में केवल दो महिलाएँ – ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और श्रीमती रेखा गुप्ता (दिल्ली, 20 फरवरी, 2025 से) – मुख्यमंत्री हैं।
लंबे समय तक केरल, बंगाल और त्रिपुरा में वामपंथी दल सत्ता में रहे। वर्तमान में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सरकार है। आज तक वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकारों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सहित वामपंथी आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही है। यह स्पष्ट है कि चाहे वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) हो, भाजपा नीत एनडीए हो, या कांग्रेस नीत यूपीए हो, सभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ये दल महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने या सहभागिता देने के लिए तैयार नहीं हैं। इनके वादे खोखले और महज बयानबाजी प्रतीत होते हैं। यही मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री पद की दृष्टि से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण सबसे निचले स्तर पर है। परिणामस्वरूप, महिलाएँ केवल मूक दर्शक बनकर रह गई हैं।
राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: लैंगिक अंतर
दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारत की राज्य विधानसभाओं में बिहार (10.70%), छत्तीसगढ़ (14.44%), और हरियाणा (10%) में 10% से अधिक महिला विधायक हैं। झारखंड (12.35%), पंजाब (11.11%), राजस्थान (12%) उत्तराखंड (11.43%), उत्तर प्रदेश (11.66%), पश्चिम बंगाल (13.70%), और दिल्ली (11.43%) भी इस सूची में शामिल हैं।
9 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा को बताया कि 19 राज्य विधानसभाओं – आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि में 10% से भी कम महिला विधायक हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के राज्य गुजरात में केवल 8.2% महिलाएँ विधानसभा के लिए चुनी जाती हैं। 68 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में केवल एक महिला, रीना कश्यप, विधायक हैं।
नागालैंड की स्थापना के बाद, 2023 तक विधानसभा के 13 चुनावों में एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं चुनी गई थी। मार्च 2023 के चुनावों में पहली बार एनडीपीपी की दो Anglia – सुश्री हेकानी जखालु और सुश्री साल्होतुनुओ क्रूस – चुनी गईं। भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे असंख्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहाँ से आज तक कोई महिला विधायक निर्वाचित नहीं हुई। संक्षेप में, विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व 20% से भी कम है।
हरियाणा की महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी रोचक है। सन् 1966 से सन् 2024 तक हरियाणा के करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, और सोनीपत जिलों से एक भी महिला लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हुई। इतना ही नहीं, इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी भी शायद ही चुनाव लड़ती हों। उदाहरण के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के नारे पर बल देती है, फिर भी सन् 2019 के चुनाव में केवल 52 विधानसभा क्षेत्रों में महिला प्रत्याशी थीं। अर्थात्, 48 निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी महिला प्रत्याशी नहीं थी। जब तक महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, तब तक महिला सशक्तिकरण के दावे खोखले और जुमले ही रहेंगे। क्योंकि राजनीतिक शक्ति के बिना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है।
लोकसभा, राज्य सभा और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रतिपक्ष की महिला नेता: लैंगिक अंतर
भारत में पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल, 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी। 73 वर्षों में केवल दो महिलाएँ – श्रीमती सुषमा स्वराज (भाजपा नीत एनडीए) और श्रीमती सोनिया गांधी (कांग्रेस नीत यूपीए) – लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। इन दोनों महिला नेताओं ने लोकसभा में विपक्षी नेता के रूप में जो भूमिका निभाई, वह अत्यंत प्रशंसनीय है।
अब तक विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं में 13 महिलाएँ प्रतिपक्ष की नेता रही हैं। अरुतला कमला देवी (स्वतंत्रता सेनानी, निजाम हैदराबाद के खिलाफ तेलंगाना शस्त्र आंदोलन की महिला नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता) आंध्र प्रदेश में प्रतिपक्ष की नेता (1 मार्च, 1964 से 1 मार्च, 1967 तक, 3 वर्ष 8 दिन) रही हैं। अरुतला कमला देवी भारत की किसी भी विधानसभा में प्रतिपक्ष की पहली महिला नेता थीं। वर्तमान में समस्त भारत में भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता (23 फरवरी, 2025 से) हैं।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के स्पीकर: लैंगिक अंतर
लोकसभा के 17 अध्यक्षों में 17 अप्रैल, 1952 से आज तक केवल दो महिलाएँ स्पीकर रही हैं। मीरा कुमार (15वीं लोकसभा, 1 जून, 2009 से 11 जून, 2014, कांग्रेस पार्टी) को पहली महिला स्पीकर होने का श्रेय प्राप्त है, और श्रीमती सुमित्रा महाजन (16वीं लोकसभा, जून 2014 से जून 2019, भाजपा) दूसरी महिला स्पीकर रही हैं। मार्च 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के विभिन्न देशों की संसदों में 22.43 प्रतिशत महिला स्पीकर हैं, जबकि भारत में इस समय दोनों सदनों में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज तक राज्य सभा में कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही। 6 दिसंबर, 1966 को शन्नो देवी (कैथल) ने नवनिर्मित राज्य हरियाणा की विधानसभा और भारत की पहली महिला स्पीकर का पद संभालने का सौभाग्य प्राप्त किया।
सन् 1950 से सन् 2025 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति: लैंगिक अंतर
सन् 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद अब तक 18 राष्ट्रपतियों (तीन कार्यवाहक राष्ट्रपतियों सहित) में से केवल दो महिलाएँ राष्ट्रपति बनी हैं – भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012) और दूसरी वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (25 जुलाई, 2022 से वर्तमान तक)। अर्थात्, सन् 1950 से सन् 2025 तक लैंगिक अंतर 18:2 है।
भारत में उपराष्ट्रपति का पद भी है (संविधान के अनुच्छेद 63-73), जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सन् 1950 से सन् 2025 तक 14 उपराष्ट्रपति इस पद पर रह चुके हैं। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से एक भी महिला इस पद पर निर्वाचित नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि लैंगिक अंतर 14:0 है।
प्रधानमंत्री का पद: लैंगिक अंतर – 14:1
संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे।
15 अगस्त, 1947 से अब तक भारत में 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (15 अगस्त, 1947 से 27 मई, 1964) का कार्यकाल आज भी भारतीय इतिहास में सबसे लंबा है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सन् 1996 में केवल 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी (नरेंद्र मोदी) भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं (30 मई, 2014 से वर्तमान तक)। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के नेता डॉ. मनमोहन सिंह (अल्पसंख्यक धर्म – सिख) 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे (सन् 2004 से सन् 2014)। हालाँकि, अब तक पिछड़े वर्ग (एच. डी. देवगौड़ा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) से दो प्रधानमंत्री बने हैं।
लेकिन भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह (मुस्लिम धर्म), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन सका। सन् 1947 से आज तक, 77 वर्षों में केवल एक महिला, श्रीमती इंदिरा गांधी, इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन हुई हैं (पहली बार सन् 1966-1967 और दूसरी बार सन् 1980-1984)। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण (जुलाई 1971), प्रिवी पर्स की समाप्ति, भारत-पाक युद्ध (सन् 1971) में जीत, बांग्लादेश का निर्माण, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण, भूमिगत परमाणु परीक्षण (सन् 1974), और सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाना (सन् 1975) शामिल हैं। इन अतुलनीय उपलब्धियों के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम विश्व इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और अंतरराष्ट्रीय नेताओं की आकाशगंगा में ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा।
भारतीय मंत्रिपरिषद: लैंगिक अंतर – पुरुष 89.53% : महिला 10.53%
सन् 1947 से लेकर आज तक भारतीय मंत्रिपरिषद में बहुत बड़ा लैंगिक अंतर रहा है। महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। भारतीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सन् 1947 में 2.63%, 1957 में 6%, 1964 में 9.8%, 1967 में 7.25%, 1980 में 7.50%, और 1984 में 11.93% था। सन् 1991 में 12%, 1997 में 11.36%, 1999 में 11.43%, 2009 में 13.79%, 2014 में 15.6%, 2019 में 10.53%, और भाजपा नीत एनडीए सरकार (03) में जून 2024 में 9.7% रहा। भाजपा नीत एनडीए सरकार (जून 2024) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 72 सदस्यों में से केवल 7 महिलाएँ मंत्री हैं।
आश्चर्यजनक किंतु सत्य यह है कि भाजपा नीत एनडीए सरकार में एक भी मुस्लिम महिला या पुरुष मंत्री नहीं है, क्योंकि एनडीए ‘मुस्लिम मुक्त’ है। लगभग 14 प्रतिशत मुस्लिम आबादी का सत्ताधारी गठबंधन में प्रतिनिधित्व न होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसका अर्थ है कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ केवल एक नारा है, जो वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। सन् 1947 से 2025 तक भारतीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 10.53% है।
सन् 1947 से 2025 तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल चार गुना बढ़ी है। यदि मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसी धीमी गति से बढ़ता रहा, तो महिलाओं को अच्छे दिन देखने में 150 साल लग जाएँगे और उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। मंत्रिपरिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यह सिद्ध करता है कि पुरुष प्रधान सोच हावी है। पुरुष ‘सत्ता के केंद्र’ में बने रहना चाहते हैं और महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार नहीं हैं। महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुसार शक्ति और स्थान दिया जाना चाहिए।
विश्व स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व: लैंगिक अंतर
विश्व स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व न केवल संसदों में, बल्कि कार्यकारी स्तर पर भी बढ़ रहा है। 1 जनवरी, 2025 के आँकड़ों के अनुसार, 25 देशों में महिलाएँ राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हैं। एक अनुमान के अनुसार, 113 देशों में आज तक एक भी महिला राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष नहीं रही।
यद्यपि वैश्विक स्तर पर मंत्रिमंडलों और मंत्रि परिषदों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 जनवरी, 2025 को प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, विश्व के विभिन्न देशों की मंत्रि परिषदों में 22.9% महिलाएँ हैं। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केवल 7 महिलाएँ हैं और मंत्रिमंडल में केवल दो महिलाएँ हैं। विश्व में केवल नौ देशों में 50% या इससे अधिक महिलाएँ मंत्रिमंडलों में हैं।
लेकिन जहाँ तक विभागीय नेतृत्व का सवाल है, लैंगिक अंतर मौजूद है। महिला विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वदेशी लोगों, और अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित विभागों में अधिक महिलाएँ शीर्ष पदों पर हैं। लेकिन सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, ईंधन, खनन, और परिवहन के क्षेत्रों में विभिन्न देशों के मंत्रिमंडलों और मंत्रि परिषदों में शीर्ष पदों पर महिलाएँ बहुत कम हैं। इसके विपरीत, वैश्विक स्तर पर वित्त, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेश विभाग, और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है। पितृसत्तात्मक मानसिकता सहित अनेक कारणों के परिणामस्वरूप पुरुषों का वर्चस्व स्थापित है और राष्ट्रीय मंत्रिमंडलों में महिलाएँ पीछे हैं।
भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व: लैंगिक अंतर
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन भारतीय संसद (लोकसभा और राज्य सभा) और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक है। सन् 1951-1952 से 2024 तक 18 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। पहले आम चुनाव (1951-52) में लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 22 थी, जो कुल सीटों (499) का केवल 4.4% थी। 15वीं लोकसभा चुनाव (2009) से 2019 तक लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगातार वृद्धि हुई।
15वीं लोकसभा (2009) में 59 महिला सांसद थीं, जो कुल सांसदों (545) का 10.9% थीं। 16वीं लोकसभा (2014) में 61 महिला सांसद थीं, जो कुल सांसदों का 11.2% थीं। 17वीं लोकसभा (2019) में 78 महिलाएँ चुनाव जीतीं, जो कुल सांसदों का 14.6% थीं। लेकिन 18वीं लोकसभा (2024) में 74 (13.6%) महिला सांसद हैं, जो सन् 2019 के लोकसभा चुनाव की महिला सांसदों की संख्या से चार कम है।
वैश्विक रैंकिंग में भारत का 152वाँ स्थान – चीन और पाकिस्तान से भी कम
भारत में पहले लोकसभा चुनाव (1951-52) से 17वीं लोकसभा चुनाव (2019) तक सात दशकों में केवल 690 महिलाएँ लोकसभा के लिए चुनी गई हैं, जिनमें से मुस्लिम महिलाओं की संख्या केवल 25 है। वर्तमान में लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या (74) 13.6% है। हालाँकि हम दावा करते हैं कि भारत दुनिया का ‘सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी’ है, लेकिन सन् 2014 में विश्व रैंकिंग में महिला प्रतिनिधियों के मामले में 193 देशों की सूची में भारत 149वें स्थान पर था।
1 फरवरी, 2025 के आँकड़ों के अनुसार, 185 देशों की सूची में भारत का स्थान 152वाँ है। अर्थात्, सन् 2014 की रैंकिंग से हम तीन स्थान नीचे खिसक गए। इसके विपरीत, विश्व महिला रैंकिंग में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 17% महिला सांसदों के साथ 137वें स्थान पर और चीन 26.5% महिला सांसदों के साथ 93वें स्थान पर है। विश्व महिला रैंकिंग में 63.8% के आँकड़ों के साथ रवांडा प्रथम स्थान पर है। 1 फरवरी, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 26.5% है, जो भारत (13.6%) से 12.9% अधिक है। लेकिन विश्व स्तर पर पुरुष प्रतिनिधित्व 73.5% और महिला प्रतिनिधित्व 26.5% है।
महिलाओं के मार्ग में आने वाली बाधाएँ
विश्व में महिलाओं के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा समाज की रुग्ण मानसिकता है। भारत का समाज पुरुष प्रधान होने के कारण ‘सन स्ट्रोक’ (पुत्र मोह) से ग्रस्त है। समाज की सोच महिलाओं के प्रति नकारात्मक और महिला-विरोधी है। सैद्धांतिक रूप से समाज में महिलाओं को देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, और दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, लेकिन व्यवहार में लड़कियों का ‘कोख में कत्ल’ कर दिया जाता है। महिलाओं का गर्भाशय बच्चा पैदा करने का स्थान न होकर ‘कब्रिस्तान’ बन गया है। कोख में कत्ल को चीन में हुए अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में ‘नरसंहार’ कहकर आलोचना की गई थी।
भारतीय समाज में महिला-विरोधी मानसिकता जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, अनपढ़ता, शिक्षित होने के बावजूद अज्ञानता, पिछड़ापन, गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति, राजनीति में प्रवेश करने वाली महिलाओं का चरित्र हनन, लैंगिक हिंसा, समाज का अनुदारवादी दृष्टिकोण, महिलाओं पर परिवार का दायित्व, राजनीतिक दलों और राजनेताओं का महिला-विरोधी दृष्टिकोण, राजनीतिक दलों में शीर्ष स्थानों पर कुछ अपवादों को छोड़कर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, राजनीतिक संप्रदायवाद, धर्मांधता, राजनीति में बाहुबल, कपट, छल, धन, गुंडागर्दी, और प्रपंच का सामान्य होना आदि मुख्य कारण हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राजनीतिक दल में परिवारवाद विद्यमान है। परिवारवाद के कारण राजनीतिक दलों द्वारा परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को टिकट दिलवाया जाता है। सामान्य कर्मठ, वफादार, और जुझारू महिला कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता। इसलिए महिलाएँ राजनीति में जाने से संकोच करती हैं। भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में राष्ट्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जाता है। यही सब लैंगिक अंतर के मूल कारण हैं।
महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सुझाव
महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विश्व के विभिन्न देशों में कई तरीके अपनाए गए हैं। 100 से अधिक देशों में संवैधानिक संशोधनों और कानूनों के जरिए महिलाओं के लिए विधायिकाओं में कोटा निर्धारित किया गया है। भारत में संसद और विधानसभाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था संबंधी अधिनियम (2023) पारित किया गया है, परंतु यह अभी लागू नहीं हुआ है। यद्यपि पंचायती राज स्तर पर 21 राज्यों और दो केंद्र शासित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनेक कमियों के बावजूद यह एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है।
संवैधानिक आरक्षण और कानूनों के साथ-साथ महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए राजनीतिक दलों को अपने संगठनों में ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कोटा निर्धारित करना चाहिए। ऐसा कानून बनाना जरूरी है कि यदि राजनीतिक दल अपने संगठनों में और टिकट वितरण के समय निर्धारित कोटे की अवहेलना करें, तो चुनाव आयोग उनकी मान्यता समाप्त कर दे।
भारत में कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के साथ-साथ समाज की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। जितना अधिक महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, उतना ही राष्ट्र मजबूत होगा। क्योंकि अधिकांश महिलाएँ समझदार, संवेदनशील, सहयोगी, समन्वयक, और सद्भावना से परिपूर्ण होती हैं। महिला राजनीतिक सशक्तिकरण का सर्वोत्तम उदाहरण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। बांग्लादेश के निर्माण में जिस तरह उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के विरोध के बावजूद भारतीय सेना के सहयोग से सफलता प्राप्त की, वह विश्व के लिखित इतिहास में अतुलनीय है।
अंततः, महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुसार शक्ति और स्थान दिया जाना चाहिए। अतः उद्घोष यह होना चाहिए – ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’। तभी लैंगिक असमानता समाप्त होगी और ‘पुरुष-केंद्रित’ व ‘पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं’ की दुनिया में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव होगा।
(डॉ. रामजी लाल सामाजिक वैज्ञानिक और करनाल स्थित दयाल सिंह कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य हैं।)