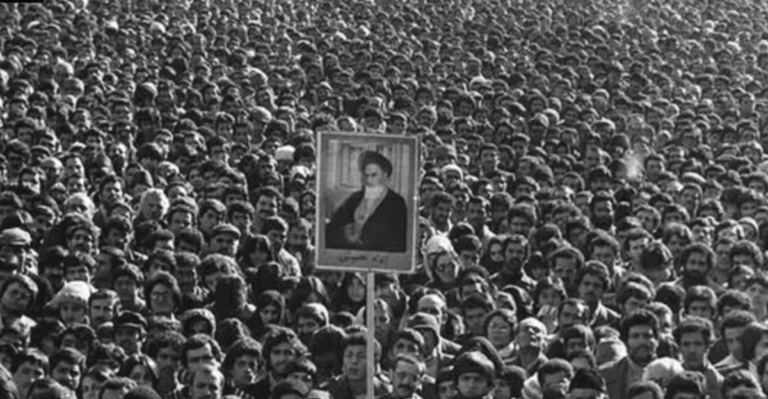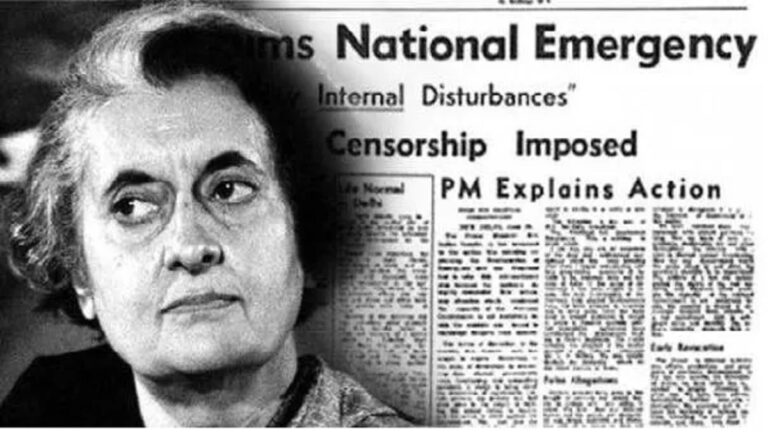जिन्होंने खुद आडवाणी को अपने रास्ते से हटाकर, एक तरह से उन्हें कारावासी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, वे आज गांधी के पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं!!
कौन नहीं जानता जिनकी वजह से वे आज एक हैसियत में हैं, उसी के लिए उन्होंने मार्गदर्शक मंडल ईजाद किया और अब दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं।
हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी राय दी थी, बावजूद इसके नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया।
हालांकि यहां भी वे सुविधावादी दृष्टि अपनाते हुए गांधी को नहीं, वरन नेहरू को ही कठघरे में खड़ा करते हैं। क्योंकि नेहरू का चरित्र हनन करने के उसके अपने लाभ हैं। गांधी का चरित्र हनन करने का काम उन्होंने अपने पार्टी वालों को दे रखा है।
यहां बताते चले कि वह चुनाव, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था, न कि प्रधानमंत्री के पद का।
नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गांधी की पसंद थे, सो वे अध्यक्ष बने।
यहां झूठ पर झूठ बोला जा रहा है और वह भी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में।
अरे भाई इतिहास में कब प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस कमेटियों से राय ली गई ? कहीं लिखा हो तो दिखाइए। जो राय ली गई थी, वह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए थी न कि प्रधानमंत्री पद के लिए।
कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव आचार्य कृपलानी नेहरू के चुने जाने पर लिखते हैं कि-“पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्ज़ी का काम यंत्रवत कर रहा था और उस वक्त मुझे ये बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आख़िर ये एक अध्यक्ष का ही तो चुनाव था।”
जब कृपलानी जैसे बड़े नेता इस घटना (कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव) को सिर्फ अध्यक्ष से जोड़कर देख रहे थे, तब आप प्रांतीय कमेटियों के साधारण नेताओं से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद के लिए ही वोटिंग की थी।
अगर मान भी लिया जाय कि उस समय अध्यक्ष बनने वाला शख्स ही प्रधानमंत्री बनता, तब भी यह बात कम से कम प्रांतीय कमेटियों के नेताओं को तो नहीं ही पता थी। यह इन टिप्पणियों से भी साफ हो जाता है।
इसके अलावा नेहरू के जीवनीकारों में से एक माइकल ब्रेचर लिखते हैं:
“अध्यक्षता को बारी-बारी से बदलने की पुरानी परंपरा के अनुसार, पटेल इस पद के लिए चुने गए थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्हें पंद्रह साल हो चुके थे, जबकि नेहरू ने 1936 और 1937 में लखनऊ और फिरोजपुर में अध्यक्षता की थी।
इसके अलावा, पटेल प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते थे। नेहरू का ‘चुनाव’ गांधी के हस्तक्षेप के कारण हुआ था।”
यहां भी बारी-बारी से अध्यक्ष पद के बदलाव का ही हवाला दिया गया है। और फिर इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया जाय कि प्रांतीय कमेटियां नेहरू के विरुद्ध थीं।
चूंकि नेहरू पहले ही तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, तो कांग्रेस समितियों ने इस बार पटेल को तरजीह दी।
इन टिप्पणियों को देखने पर सहज ही यह कहा जा सकता है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के पद का संदर्भ तो कहीं था ही नहीं।
इसके अलावा पटेल के अनन्य सहयोगी और महाकौशल के बड़े नेता द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने अपनी किताब में यह ज़िक्र किया है कि “पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने सिफारिश करते समय नेहरू को प्रधानमंत्री पद से वंचित किए जाने की बात किसी के दिमाग में नहीं थी।”
पटेल की बढ़ती उम्र और प्रांतीय कमेटियों से उनका जुड़ाव उनके चुने जाने का प्रमुख कारण बना। वे नेहरू की तुलना में ज्यादा जमीनी नेता थे या कह सकते हैं कि वे पार्टी के अन्य नेताओं के लिए ज्यादा सुलभ रहते हों।
अब प्रश्न उठता है आख़िर ऐसी बातें क्यों? क्या उस समय नेहरू को पटेल का प्रतिद्वंद्वी माना जाता था, जो ऐसी बातें की जा रहीं हैं?
अगर नेहरू और पटेल के संबंधों को समझना है तो दोनों के मध्य हुए पत्राचार को देखना चाहिए। इस संदर्भ में एकाधिक पत्रों का उल्लेख करना समीचीन होगा।
पहले मंत्रिमंडल के गठन हेतु जब नेहरू औपचारिकतावश पटेल को पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा देखिए और उससे भी ज्यादा उस पत्र की भाषा देखिए जो पटेल ने प्रत्युत्तर में लिखा।
1 अगस्त 1947 को नेहरू पटेल को लिखते हैं-
”कुछ हद तक औपचारिकताएं निभाना ज़रूरी होने से मैं आपको मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने के लिए लिख रहा हूं। इस पत्र का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप तो मंत्रिमंडल के सुदृढ़ स्तंभ हैं।’
जवाब में पटेल ने 3 अगस्त को नेहरू को लिखा-
”आपके 1 अगस्त के पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। एक-दूसरे के प्रति हमारा जो अनुराग और प्रेम रहा है तथा लगभग 30 वर्ष की हमारी जो अखंड मित्रता है, उसे देखते हुए औपचारिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आशा है कि मेरी सेवाएं बाकी के जीवन के लिए आपके अधीन रहेंगी।
आपको उस ध्येय की सिद्धि के लिए मेरी शुद्ध और संपूर्ण वफादारी औऱ निष्ठा प्राप्त होगी, जिसके लिए आपके जैसा त्याग और बलिदान भारत के अन्य किसी पुरुष ने नहीं किया है। हमारा सम्मिलन और संयोजन अटूट और अखंड है और उसी में हमारी शक्ति निहित है। आपने अपने पत्र में मेरे लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।”
इसके अलावा 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में पटेल ने अपने भाषण में कहा-
“अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं हैं, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूं।”
अब इन बयानों को पढ़िए और फिर बताइए कि क्या वाकई दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी?
क्या वाकई इन नेताओं में मध्य पदलिप्सा का कोई भाव था?
जब पटेल खुद गांधी के निर्णय को बिना किसी संकोच के खुलकर स्वीकारने को अपना धर्म बता रहे हैं, तो फिर उनकी तरफ से पैरवी का औचित्य क्या? क्या भारत के लौह पुरुष को आपकी पैरवी की जरूरत पड़ेगी?
और पटेल ही क्यों, कांग्रेस में गांधी का निर्णय तो सभी स्वीकारते थे और यह सहमति कांग्रेसियों ने गांधी जी को स्वेच्छा से दे रखी थी। गांधी के पास दबाव डालने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी कोई संस्था नहीं थी।
जाहिर है ये बातें इसलिए की जाती हैं कि नेहरू को गरियाने के अपने राजनीतिक लाभ हैं। खैर नैतिक मूल्यों की राजनीति की अपेक्षा है भी नहीं।
ज्ञात हो कि गांधी जी 1942 में ही नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, बावजूद इसके नेहरू कई बार गांधी जी की राय से सहमत नहीं होते थे और वे अपनी नाइत्तफाकी को खुलकर जाहिर भी करते थे। स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध शीर्ष नेतृत्वकर्ता वैचारिक भिन्नता की अभिव्यक्ति का सदैव स्वागत करते थे।
गांधी ने बिना लाग-लपेट के इस चुनाव में ये साफ़ कर दिया था कि ‘अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा, इसके कई कारण हैं। उनका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता।’
वे नेहरू को लेकर बहुत स्पष्ट थे। हालांकि बाद में गांधी ने एक जगह इस बारे में कहा था – ‘जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथ से ली जा रही हो, उस समय कोई दूसरा आदमी नेहरू की जगह नहीं ले सकता। वे हैरो के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेज़ों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं।’ (महात्मा, तेंदुलकर खंड 8 पेज 3)
नेहरू का वैश्विक कद प्रधानमंत्री बनने में प्रभावी हुआ। उस समय अगर कांग्रेस के बाहर भी किसी अन्य दल से पूछा जाता तो वह भी नेहरू की ही संभावना जताता। विदेशों में भी नेहरू ही भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते थे।
झूठ बोलने का इतिहास रचकर आप नैतिकता की दुहाई देते हैं। हद है!
क्या आपके यहां अध्यक्ष के चुनावों में प्रांतीय कमेटियों की राय ली जाती है? क्या इस तरह के चुनावों की विधिवत परंपरा है आपकी पार्टी में? यदि नहीं तो आपको कोई नैतिक आधार नहीं इस तरह की बातें करने का।
खैर छोड़िए जब आप समकाल न होते हुए भी गुरु गोरखनाथ जी की नानक और कबीर से उनकी आमने-सामने मुलाकात और संवाद करा सकते हैं और तक्षशिला को बिहार में बता सकते हैं, तो ये तो सब छोटी बातें हैं आपके लिए।
(संजीव शुक्ल स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)