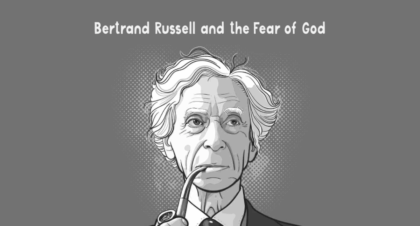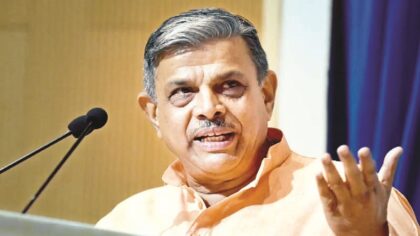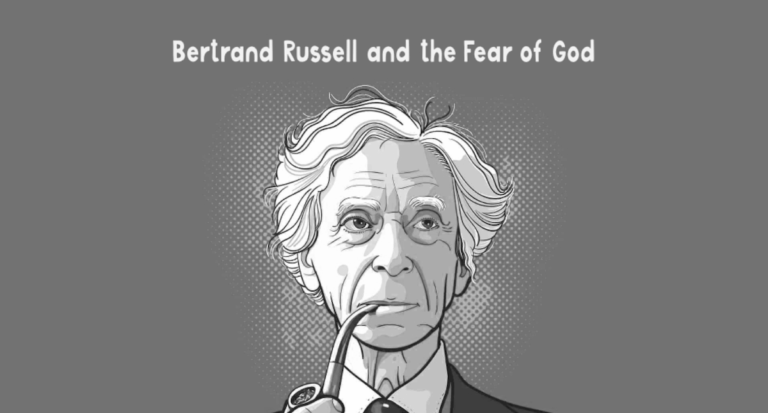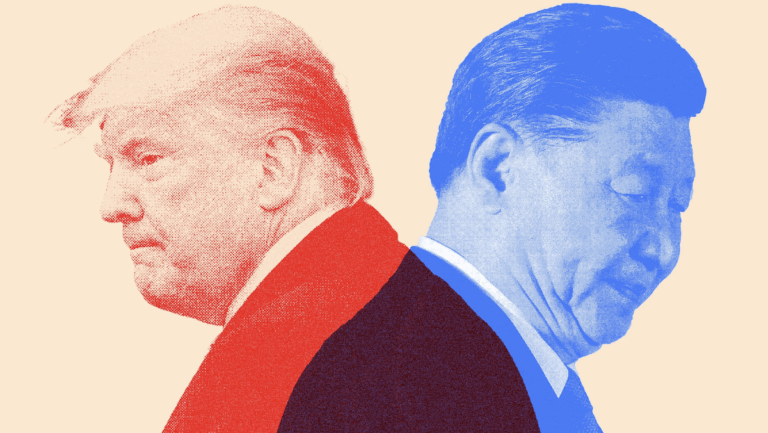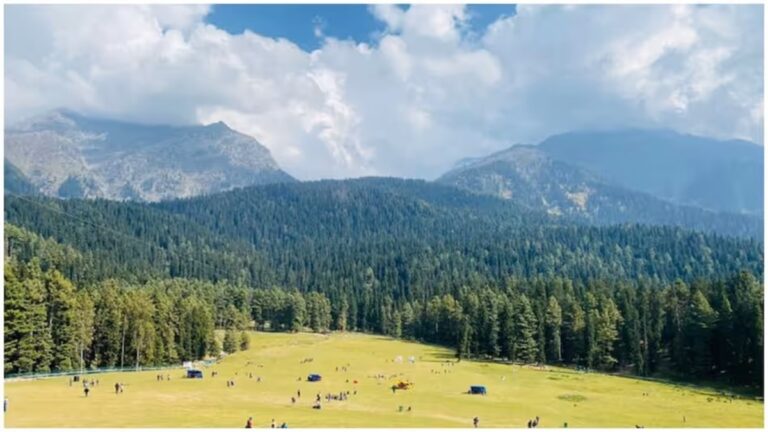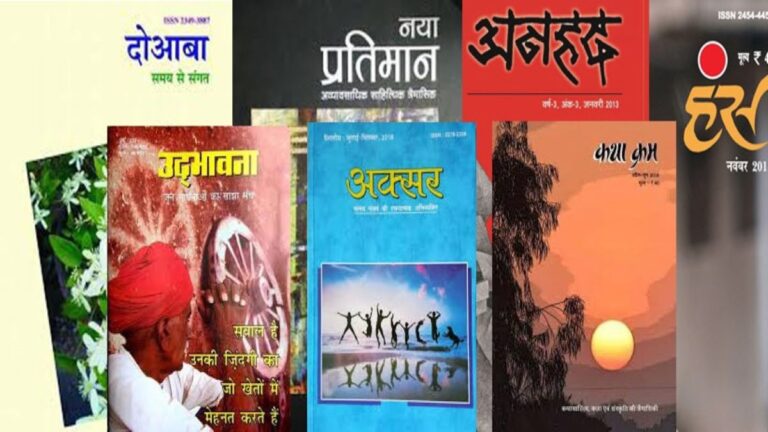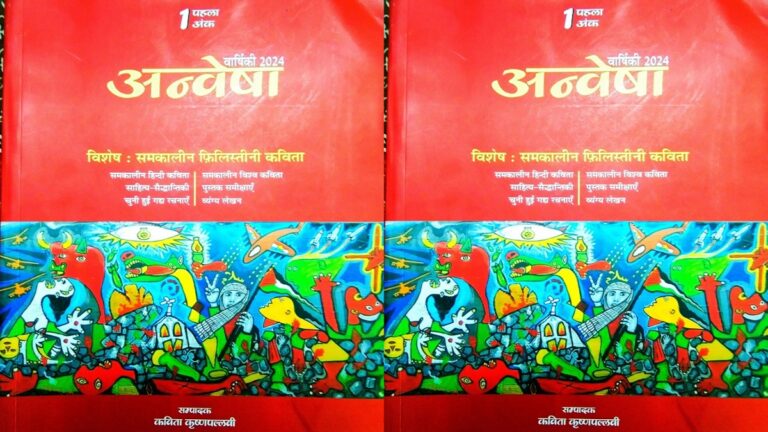किसान आत्महत्याओं के बारे में जानने के लिए इसका इतिहास जान लेना भी आवश्यक है। और इसे महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में जानना तर्कसंगत होगा। सन 1990 में अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ के ग्रामीण मामलों के संवाददाता पी. साईंनाथ ने किसानों द्वारा नियमित आत्महत्याओं की सूचना दी। आरंभ में ये रपटें महाराष्ट्र से आईं। जल्दी ही आंध्रप्रदेश से भी आत्महत्याओं की खबरें आने लगीं। शुरुआत में लगा कि अधिकांश आत्महत्याएं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों ने ही की हैं। लेकिन महाराष्ट्र के राज्य अपराध लेखा कार्यालय से 2010 में प्राप्त आंकड़ों को देखने से स्पष्ट हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में कपास सहित अन्य नकदी फसलों के किसानों की आत्महत्याओं की दर बहुत अधिक रही है।
आत्महत्या करने वाले केवल छोटी जोत वाले किसान नहीं थे बल्कि मध्यम और बड़े जोतों वाले किसान भी थे। राज्य सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए कई जाँच समितियाँ बनाईं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्य सरकार द्वारा विदर्भ के किसानों पर व्यय करने के लिए 110 अरब रूपए के अनुदान की घोषणा की। बाद के वर्षों में कृषि संकट के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने आत्महत्याएँ की। इस दृष्टि से 2009 में भारत के राष्ट्रीय अपराध लेखा कार्यालय ने 17368 किसानों के आत्महत्या की रपटें दर्ज कीं। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई थी। इन 5 राज्यों में 10765 यानी 62% आत्महत्याएँ दर्ज हुईं।
गत दशक के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में हर साल औसतन तीन हजार किसान आत्महत्या करते हैं। वर्ष 2020 में दो हजार 270 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। हालांकि, यह वर्ष 2019 के मुकाबले 262 कम है। इस साल राज्य के कोकण में अंचल में आत्महत्या नहीं हुई। ये आंकड़े राज्य के राहत व पुनर्वास विभाग ने सूचना के अधिकार द्वारा मांगी गई जानकारी में दिए। हालांकि, इन आंकड़ों को जारी करते हुए विभाग ने दावा किया कि वर्ष 2020 में नागपुर और नासिक संभाग को छोड़ दें तो सभी संभागों में किसान आत्महत्या के प्रकरण कम हुए हैं। विदर्भ राज्य में किसानों की आत्महत्या के लिए पहचाना जाता है। आत्महत्या करने के बाद सरकार की तरफ से किसान परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। लेकिन, आत्महत्या करने से पहले ही इन आत्महत्याओं के मूल में छिपे कारण को सुलझाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।
राज्य के इस अंचल में पिछले साल एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में किसानों के मानसिक अवसाद को समझने की कोशिश की गई थी। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि विदर्भ के साठ प्रतिशत किसानों को मानसिक उपचार की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण को करने वाली संस्था ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पॉपुलेशन साइंस’ का मानना था कि विदर्भ के किसानों को मानसिक परामर्श देने के लिए सरकार आगे आए और उनके लिए विशेषज्ञ और प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करे। इस सर्वेक्षण में विदर्भ के 34.7 प्रतिशत किसानों में गंभीर मानसिक बीमारियों से जुड़े लक्षण पाए गए थे। इनमें 55 प्रतिशत किसानों की स्थिति चिंताजनक थी। वहीं, 24.7 प्रतिशत किसान जबरदस्त हताशा से गुजर रहे थे।
प्रश्न है कि विदर्भ के किसान मानसिक अवसाद की स्थिति से क्यों गुज़र रहे हैं। दरअसल, विदर्भ की एक बड़ी आबादी पूरी तरह खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है और आजीविका के लिए खेती ही एक विकल्प है। या दूसरे शब्दों में यहां के लोगों के पास खेती का विकल्प नहीं है। लेकिन, इसे विडंबना ही कहेंगे कि विदर्भ की इतनी बड़ी आबादी की आजीविका मानसून पर निर्भर है।
आंकड़ों के मुताबिक यदि यहां की 91 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है तो ज़ाहिर है कि मानसून की अनिश्चितता उनके जीवन को प्रभावित करती है। हालांकि, विदर्भ की खेती पर छाया संकट सिर्फ मानसून पर निर्भरता के कारण ही नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकार की गलत नीति, बढ़ती लागत और राजनैतिक नेतृत्व द्वारा किसानों के प्रश्नों पर बरती जाने वाली उदासीनता भी जिम्मेदार है। फिर विदर्भ में किसानों को ऋण देने वाली विश्वसनीय संस्थाओं का अकाल है। लिहाजा, अब भी यहां के किसान पैसे के लिए साहूकारों के सहारे ही हैं।
इसी तरह, विदर्भ की खेती का यह संकट मुख्यत: बेमौसम बरसात के साथ कपास जैसे नकद फसल को उगाने वाली खर्चीली खेती से भी जुड़ा है। इसे इस साल किसानों पर आई ताजा आफत से भी समझ सकते हैं।
चिंता की बात है कि यह लगातार दूसरा साल है जब खराब मौसम और अनियमित बरसात के कारण यहां कपास की फसल बर्बाद हुई है।
दरअसल, कपास की पैदावार के मामले में महाराष्ट्र का विदर्भ अंचल अग्रणी रहा है। बीते साल हालत यह रही कि यहां खरीफ मौसम की इस फसल को उगाने वाले किसानों ने 60 प्रतिशत तक घाटा सहा है। यही वजह है कि यहां के किसानों का बजट गड़बड़ा गया है। जाहिर है कि इस आर्थिक नुकसान का असर उनके आगामी सीजन पर भी पड़ेगा।
विदर्भ में खास तौर से यवतमाल जिले को कपास उत्पादन के कारण जाना जाता है। लेकिन, पिछले कई वर्षों से विदर्भ के अन्य जिलों की तरह यवतमाल जिला भी किसान आत्महत्याओं के कारण चर्चा में रहा है। ऐसा इसलिए कि यहां पिछले कुछ दशकों से कृषि क्षेत्र में आए संकट के भंवरजाल में फंसे किसान इससे बाहर नहीं निकल पा रहे है। इसके बावजूद यहां के किसान मौजूदा परिस्थितियों को बदलने के लिए हर साल लगातार अपने खेतों में बुवाई कर रहे है।
प्रश्न है कि विदर्भ का एक कपास उत्पादक किसान बंपर फसल की उम्मीद पर प्रति एकड़ अपने खेत में सालाना किन-किन चीजों पर करीब कितनी लागत खर्च करता है।
अच्छी फसल लेने के लिए इन किसानों की मेहनत खेतों को समतल बनाने से शुरू होती है। इसके बाद वे खेत से कचरा निकालने के बाद बीज, खाद और कीटनाशक खरीदते हैं। फिर कुछ मजदूरों को मजदूरी देकर बुवाई करते हैं। कपास के लिए एक निश्चित अवधि में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तब जाकर जब फसल तैयार होती है तो उन्हें कपास की छटाई करनी पड़ती है। इतना करने के बाद जब वह अपना कपास खेत से ढोकर बाजार में लाता है तो माल बेचने के साथ उसे फिर कड़ी कसरत करनी पड़ती है। महीनों की मेहनत और हजारों रुपए खर्च करने के बाद जब एक छोटा किसान उसे तुरंत बेचना चाहता है तो चाहकर भी कई बार उसे उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। कारण यह है कि हर साल की तरह इस साल भी शासकीय कपास खरीदी केंद्रों पर खरीद की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसलिए अनेक किसानों ने व्यापारियों को 5,300 से लेकर 5,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कपास बेचा है।
बता दें कि यहां किसानों द्वारा खरीफ के मौसम में सबसे ज्यादा खेती कपास की ही होती है। कई किसानों ने बातचीत में बताया कि वे हर साल कपास की खेती पर प्रति एकड़ करीब 35 हजार रुपए खर्च करते हैं। पूरी लागत सामान्यत: इस प्रकार से होती है- खेत समतलीकरण पर 1,000, कचरा सफाई पर 500, बीज पर 750, रोपण पर 500, खाद पर 5,000, खरपतवार-नाशकों पर 5,000 कीट-नाशकों पर 5,000, सिंचाई पर 10,000, कपास की छटाई पर 4,000, वाहन पर 2,000 और रखवाली पर 1,000 रुपए।
हालांकि, गत वर्ष जब कपास उत्पादक किसान बंपर पैदावार को लेकर उत्साहित दिख रहे थे तो सितंबर से नवंबर और दिसंबर तक हुई बरसात ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मौसम अक्सर किसानों को धोखा देता है, फिर खेती की लागत मंहगी होती जा रही है, मगर इस पर भी किसान खेती करने से डरता नहीं है। बात यह है कि वह करे भी तो क्या! पिछली बार भी जब उसने खून-पसीना बहाकर फसल खेतों में तैयार की थी तो खूब पानी बरसा। नतीजा यह कि उसे आधे से कम फसल हासिल हुई है। इसलिए उसे आधे से अधिक घाटा लगा। लगातार घाटा सहने का एक मतलब यह है कि किसान कर्ज के बोझ के नीचे पहले से कहीं ज्यादा दब चुका होता है।
राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में हुईं किसानों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं विदर्भ के अमरावती संभाग में हुईं। इस दौरान अमरावती संभाग में सबसे अधिक एक हजार 893 किसानों के आत्महत्या से जुड़े प्रकरण सामने आए। अमरावती संभाग के यवतमाल जिले में सबसे अधिक 295 किसान आत्महत्याओं के प्रकरण उजागर हुए। दूसरे स्थान पर मराठवाडा का औरंगाबाद संभाग है, जहां इन दो वर्षों में एक हजार 528 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमश: नासिक और नागपुर संभाग हैं, जहां वर्ष 2019 के मुकाबले किसान आत्महत्याओं में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इन दो वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या नासिक और नागपुर संभाग में क्रमश: 774 और 456 है। एक ओर, राज्य सरकार का राहत व पुनर्वास विभाग वर्ष 2020 में किसान आत्महत्याओं में आई इस कमी के पीछे कुछ कारण गिना रहा है। इसका कहना है कि राज्य की महागठबंधन वाली नई सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर दिया, जिससे पिछले साल किसानों को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिली है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की ओर से भूमि राजस्व और बिजली के बिलों में भी छूट दी गई है।
भारतीय कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है तथा मानसून की असफलता के कारण नकदी फसलें नष्ट होना किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का मुख्य कारण माना जाता रहा है। मानसून की विफलता, सूखा, कीमतों में वृद्धि, ऋण का अत्यधिक बोझ आदि परिस्थितियां, समस्याओं के एक चक्र की शुरुआत करती हैं। बैंकों, महाजनों, बिचौलियों आदि के चक्र में फंसकर भारत के विभिन्न हिस्सों के किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं। किसानों को आत्महत्या की दशा तक पहुंचा देने के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में एक सबसे बड़ा कारण खेती का आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह होना तथा किसानों के भरण-पोषण में असमर्थ होना है। कृषि की अनुपयोगिता के मुख्य कारण हैं- कृषि जोतों का छोटा होते जाना – 1960-61 में भूस्वामित्व की इकाई का औसत आकार 2.3 हेक्टेयर था जो 2002-2003 में घटकर 1.6 हेक्टेयर रह गया।
भारत में उदारीकरण की नीतियों के बाद खेती (खासकर नकदी खेती) करने का तरीका बदल चुका है। सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण “पिछड़ी जाति” के किसानों के पास नकदी फसल उगाने लायक तकनीकी जानकारी का अक्सर अभाव होता है और बहुत संभव है कि ऐसे किसानों पर बीटी-कॉटन आधारित कपास या फिर अन्य पूंजी-प्रधान नकदी फसलों की खेती से जुड़ी कर्जदारी का असर बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा होता हो।
(शैलेंद्र चौहान साहित्यकार और लेखक हैं। आप आजकल जयपुर में रहते हैं।)