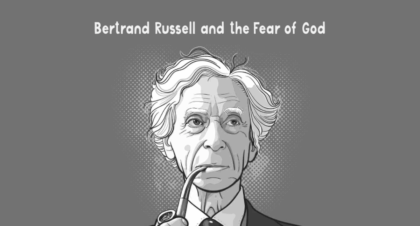कोरोना शायद पहली विपदा है जिसने मानवीय जीवन को संचालित करने वाली सभी संस्थाओं को बुरी तरह झकझोर दिया है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षा धार्मिक संस्थाओें में दिखाई दे रही है। इसके बाद नंबर आता है उदारीकरण को टिकाए रखने वाली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं और उसके साए में चलने वाली दक्षिणपंथी राजनीति का। मंदिर, मस्जिद और चर्च दूसरे मौकों पर भी बंद हुए हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि लोगों को भयमुक्त करने में धार्मिक उपदेशकों तथा कर्मकांडों की भूमिका लगभग शून्य हो गई है।
इसमें सोशल डिस्टेंसिंग ने अहम भूमिका निभाई है। एक और चीज ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। दुनिया के हर हिस्से में महामारी का फैलाव। वैश्वीकरण वाली दुनिया में स्थानीय स्तर के उपचार जिनमें धार्मिक उपचार शामिल हैं, को लोग नहीं मान सकते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रार्थना और चमत्कार का मौका मिल भी नहीं रहा है और मिल भी जाए तो उसे लोग आजमाने की स्थिति में नहीं हैं।
ऐसा नहीं है कि अपने उखड़ते हुए पांव को फिर से जमाने की कोशिशें नहीं चल रही हैं। सभी धर्म के गुरू किसी न किसी तरीके से यह काम कर रहे हैं। भारत में ही देख लीजिए। देश में जैसे ही कोरोना की बीमारी आई। बाबा रामदेव चैनलों पर दिखाई देने लगे। शुरू में तो वह यहां तक दावा करने लगे कि कोरोना के वायरस को मारने के लिए अलकोहल के उपयोग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बाद में, उन्होंने इसे कहना छोड़ दिया, लेकिन इस पर डटे रहे कि कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी प्रतिरोधक क्षमता योग के सहारे पैदा की जा सकती है। भारत में योग धार्मिक परंपरा का हिस्सा है।
इसके पक्ष में किए जाने वाले दावे चमत्कारों की श्रेणी में ही आते हैं। बाबा रामदेव हों या उच्च मध्य वर्ग के चहेते जग्गी वासुदेव, उन्होंने अपने-अपने ढंग से कोरोना से लड़ने की अपनी क्षमता बताने की कोशिश की। कोरोना के बारे में दी जाने वाली चेतावनियों को खारिज करने के यही तरीके मौलाना साद या सिख ग्रंथियोें ने किया। साद ने साफ तौर पर इन चेतावनियों को नहीं मानने की बात भी कही। लेकिन बाकी गुरूओं की तरह उन्होंने हालात की नजाकत को देखा और मेडिकल निर्देशों को मान लिया।
दुनिया के सभी धर्मस्थलों के एक साथ बंद हो जाने के बाद उनकी जमीन उतनी मजबूत नहीं रह गई है। वे निकट भविष्य में लोगों के मन में उठने इन सवालों को लेकर चिंतित हैं कि भयानक संकट के समय ईश्वरीय सत्ता के केंद्र माने जाने वाले धार्मिक स्थलों के बंद होने का वे क्या जवाब देंगे? यानि ऐसे मौकों पर उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है। उनका विश्वास हिलना अवश्यंभावी है। धर्मस्थलों और चौबीसों घंटे चलने वाले धार्मिक व्यवहारों के कई दिनों तक रूक जाने से लोगों को यह सोचने से कौन रोक सकता है कि इनके बिना भी उनका काम चल सकता है।
दक्षिण कोरिया ही नहीं, ब्राजील जैसे देशों में भी चर्च ने सरकारों के साथ असहयोग का रवैया अपनाया और उनका खुल कर विरोध किया। बीमारी का फैलाव खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बाद भी चर्च अपनी प्रार्थना सभाओं को जारी रखने की कोशिश में लगे रहे। जाहिर है कि बड़े संकट की घड़ी में वे अंतिम मददगार की अपनी भूमिका छोड़ना नहीं चाहते हैं। धार्मिक कट्टरपंथ की राजनीति करने वालों के सामने भी वही चुनौतियां हैं जैसी धर्म गुरूओं के सामने है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईस्टर में पाबंदियों में छूट देना चाहते हैं और भारत में प्रधानमंत्री मोदी रामायण और महाभारत सीरियल दिखाने के साथ-साथ योग तथा अंत:करण में झांकने की सलाह देते हैं। बीच में, दीपावली जैसा एक भव्य प्रकाश पर्व का देशव्यापी आयोजन करते हैं और मां भारती के स्मरण की बात करते हैं। हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए तबलीगी जमात को भी निशाना बनाने में उनके लोग चूकते नहीं हैं। लेकिन इस तरह के उपाय भगवान के छुट्टी पर चले जाने का जवाब नहीं दे सकते।
कोरोना ने धर्म की संस्थाओें का पांव हिलाने के साथ-साथ उदारीकरण के दौर में शक्तिशाली हुईं आर्थिक संस्थाओं के जड़ें भी हिला दी हैं। इन संस्थाओं ने धीरे-धीरे स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर आवास तथा पोषण तक-मानवीय जीवन से जुड़ी तमाम गतिविधियों की नीति तय करने का काम अपने हाथ में ले लिया था। विश्व बैंक तथा आईएमएफ जैसी संस्थाओें की भूमिका इस महामारी में शून्य नजर आ रही है। यहां संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हेल्थ आरगेनाइजेशन जैसी संस्थाएं ही अपने महत्व को फिर से साबित कर रही हैं। इन संस्थाओं की ताकत का स्रोत दूसरे विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद तथा फासीवाद के बाद लोकतंत्र के विश्वव्यापी प्रसार में है। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने मजबूत किया है।
अमेरिकी तथा यूरोपीय पूंजी के प्रसार में लगी वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ जैसी संस्थाओें के उद्देश्योें से इनका एक स्वाभाविक अंतर्विरोध रहा है। देश के स्तर पर भी हम यही देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में आर्थिक सलाहकारों तथा नीति आायोग जैसी उन संस्थाओं की कोई भूमिका नहीं है जो उदारीकरण तथा निजी पूंजी के विस्तार के लिए बनी हैं। इस काम का नेतृत्व नेहरू युग के दौरान स्थापित सार्वजनिक उपक्रम और नौकरशाही ही कर रही हैं। वेंटिलेटर्स से लेकर टेस्टिंग किट्स और वैक्सीन से लेकर दवाइयों के बारे में डीआरडीओ, आईआईटी, सीएसआईआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलाॅजी जैसी संस्थाएं ही लगी हैं।
महामारी के फैलाव की गति समझने और उसे रोकने के काम में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ही लगी है। यह सब इसके बावजूद हो रहा है कि पिछले सालों में उनके अनुदान कम कर दिए गए हैं और उनका काम छीन कर मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के हाथ में दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में निजी कंपनियां तथा अस्पताल अपना मुनाफा नहीं छोड़ रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व के स्थापित होने की इस घटना का लाभ देश की वे ट्रेड यूनियनें उठा सकती हैं जो इनका अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं।
अमेरिका, ब्रिटेन ही नहीं दुनिया के कई देशों में कोरोना से हो रही मौतों को रोकने तथा इलाज की बेहतर व्यवस्था में सामने आ रही दिक्कतों तथा नाकामी के लिए स्वास्थ्य सेवा तथा शोध के निजी हाथों में देने की नीति को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इटली की स्वास्थ्य सेवा दुनिया की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में गिनी जाती थी, लेकिन दक्षिणपंथी सरकारों ने इसे कमजोर कर दिया। उसकी कीमत उसने भारी संख्या में लोगोें की जान गंवा कर चुकाई है। अमेरिका में भी स्वास्थ्य सेवा पर जीडीपी का 17 प्रतिशत खर्च होता है, लेकिन कोरोना से लड़ने में उसका दम फूल रहा है। इसकी वजह वहां की निजी कंपनियों का दबदबा है।
वे उन्हीं शोधों में पैसा लगाती हैं और वैसे ही सुविधाएं खड़ी करती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। उन बीमारियों के इलाज में उनकी कोई रुचि नहीं होती है जो मुनाफा नहीं देती हैं। यही वजह है कि सर्वशक्तिमान अमेरिका चीन तथा भारत से सहायता मांग रहा है और क्यूबा जैसा कमजोर देश यूरोपीय देशों की मदद कर रहा है। क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह सरकार के हाथ में है और दुनिया की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा मानी जाती है। वहां सरकारी और लोगों का पैसा बीमा कंपनियों जैसे बिचौलियों तथा निजी अस्पतालों की जेब में नहीं जाता है। जाहिर है कि स्वास्थ्य सेवा के सरकारीकरण का दबाव बढ़ेगा। यह आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
मामला सिर्फ स्वास्थ्य सेवा का नहीं है। सामाजिक सुरक्षाओं को नष्ट करने का जो अभियान वैश्वीकरण तथा दक्षिणपंथ के विश्वव्यापी उभार के कारण चला था, वह कोरोना के कारण बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार जाने के बाद पीछे की ओर जाएगा।
लेकिन क्या महामारी की वजह से नए समाज के बारे में सोचने का जो अवसर मिला है उसका उपयोग बौद्धिक तथा राजनीतिक स्तर पर हो पाएगा? क्या कमजोर होते लोकतंत्र और मानवीय मूल्यों के ह्रास वाली व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के मौके का उपयोग बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा? पिछले दिनों वामपंथी राजनीति इस तरह कमजोर हुई और इसमें कल्पनाशीलता की इतनी कमी आई है कि इससे दक्षिणपंथ को परास्त करने की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। दक्षिणपंथ इतनी आसानी से मैदान छोड़ेगा भी नहीं। यह हम कोराना के समय नरेंद्र मोदी के व्यवहार में देख सकते हैं। कोरोना की डरावनी महामारी में भी अपनी छवि बनाने के रास्ते वह ढूंढ लेते हैं।
वह न तो विपक्ष का साथ लेते हैं और न ही अपने कैबिनेट के साथियों का और कोरोना की लड़ाई अकेले ही लड़ते नजर आना चाहते हैं। हर जगह मोदी ही मोदी। महामारी के दौर में भी कोई प्रधानमंत्री कितना अनैतिक हो सकता है, यह साफ दिखाई देता है। उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए उसका 25 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया है जितनी छूट उन्होेंने निजी कंपनियों को दी है। लेकिन कमजोर विपक्ष उनकी इन कमियोें को उजागर नहीं कर सकता क्योंकि वह भी उदारीकरण के खिलाफ किसी निर्णायक अभियान के लिए तैयार नहीं है। मोदी पर्सनालिटी कल्ट और सांप्रदायिकता के सहारे दक्षिण पंथ की नैया परा कराने की कोशिश में लगे हैं। देखना यह है कि वह इसमें कितना सफल हो पाते हैं।
(अनिल सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)