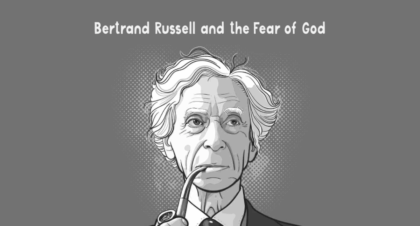विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों में बंटे समाज में कानून का शासन, ऐसी न्यायिक व्यवस्था के द्वारा ही संभव है, जिसमें सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व हो। जजों और कर्मचारियों की नियुक्तियां, विभिन्न वर्गों और संप्रदायों के बीच से, उनकी संख्या के अनुपात में हों, जिससे हर वर्ग को न्याय का चेहरा न्यायिक लगे। आजादी के पचहत्तर साल बाद, हालात कितने पक्षपातपूर्ण हैं, इसकी बानगी देखिए।
केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 21 जुलाई 2023 को लोकसभा में सूचित किया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 2018 से लेकर 17 जुलाई 2023 तक कुल 604 जजों की नियुक्तियां हुईं हैं, जिनमें ओबीसी वर्ग से 72, एस.सी. वर्ग से 18, एस.टी. वर्ग से 9 और अल्पसंख्यक वर्ग से 34 जजों की नियुक्तियां हुई हैं। इस प्रकार देश की पचासी प्रतिशत आबादी के बीच से कुल 133 गैर सवर्ण जजों की नियुक्तियां हुईं हैं जो कुल नियुक्तियों का मात्र 22 प्रतिशत हैं। वहीं शेष पन्द्रह प्रतिशत सवर्ण आबादी के बीच से कुल 454 जजों की यानी 78 प्रतिशत जजों की नियुक्तियां हुई हैं। एक लोकतांत्रिक देश के न्यायिक संस्थान का इससे ज्यादा अन्यायिक चेहरा और क्या हो सकता है?
यह स्थिति शुरू से बनी हुई है। ड़ेढ़ वर्ष पूर्व न्याय मंत्रालय द्वारा अवगत कराया गया था कि 2018 से 19 दिसम्बर 2022 तक सभी उच्च न्यायालयों में कुल 537 जजों की नियुक्तियां हुईं थीं, जिनमें 11 प्रतिशत जज ओबीसी वर्ग के, 2.8 प्रतिशत एस.सी. वर्ग के, 1.3 प्रतिशत एस.टी. वर्ग के और 2.6 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के जज थे।
डॉ. अम्बेडकर की पूरी लड़ाई वर्णवादी व्यवस्था में दलितों के प्रति अन्याय, उपेक्षा और शोषण के विरुद्ध रही। दलितों के लिए न्याय जैसी कोई अवधारणा का सृजन, वर्णवादी व्यवस्था में कभी हुआ ही नहीं। बुद्ध, सिद्ध, गोरख और कबीर, सभी ने जातिवादी वर्चस्ववाद और वंचितों के शोषण के प्रति आवाज उठाई, मगर ढीठ और धूर्त समाज ने कभी वंचितों के प्रति न्याय का समर्थन नहीं किया। उम्मीद थी कि आजादी के बाद स्थिति बदलेगी मगर ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद से हमारे न्यायालयों में वंचितों को स्थान देने पर कभी विचार ही न हुआ। नियुक्तियों में आरक्षण का वहां कोई विधान लागू न हुआ। वहां नियुक्तियों की जो प्रक्रिया कायम की गई, उसमें वंचितों को कोई स्थान मिलना ही नहीं था।
तीन दशक पहले, करिया मुण्डा समिति की रिपोर्ट ने बताया था कि 1 जनवरी 1993 तक, 18 उच्च न्यायालयों में से 12 में एक भी एस.सी. जज न था और 14 उच्च न्यायालयों में एक भी एस.टी. जज न था। 1 मई 1998 की रिपोर्ट के अनुसार भी स्थिति में कोई सुधार न हुआ और उच्च न्यायालय के कुल 481 जजों में से मात्र 15 एस.सी. और 5 एस.टी. जज नियुक्त हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति शून्य थी। वर्ष 2011 में 21 उच्च न्यायालयों में कुल 850 जज नियुक्त थे परन्तु 14 उच्च न्यायालयों में एक भी एस.सी./एस.टी. जज नियुक्त न थे। तब सर्वोच्च न्यायालय के कुल 31 जजों में से एस.सी./एस.टी. का कोई जज न था।
कहा जाता है कि वंचित वर्गों के योग्य और वरिष्ठ वकील नहीं मिलते, जिन्हें जजों की नियुक्ति हेतु संस्तुति किया जाए। इस बात में सच्चाई नहीं है। उच्च न्यायालयों में वंचित वर्गों के तमाम वरिष्ठ और योग्य वकील लम्बे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं मगर उनका नाम जजों की नियुक्ति हेतु नहीं भेजा जाता। पहली बात तो आजतक बार एसोसिएशनों में एस.सी, एस.टी. और ओ.बी.सी. वकीलों की कोई सूची बनी ही नहीं है। ऐसे आंकड़े रखे ही नहीं जाते हैं। दूसरी बात यह कि जब जजों के बेटे ही उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर है उन्हीं के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसले होंगे और उन्हीं का रिकार्ड बेहतर माना जायेगा।
हमारी न्यायिक संस्थानों का वर्ग चरित्र सवर्णवादी रहा है। अंग्रेजों के आने के पूर्व जो न्याय की अवधारणा थी, वह अन्यायिक थी और एक जाति विशेष को ही न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। मुनस्मृति जैसे ग्रंथों के तमाम विधान इतने अमानवीय हैं कि डॉ. अम्बेडकर को उसे जलाने का निर्णय लेना पड़ा था। हमारे यहां न्याय की अवधारणा वहीं से प्रेरित है। कहना न होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में मनु की मूर्ति अकारण नहीं लगाई गई है।
आजादी के बाद उम्मीद थी कि पचासी प्रतिशत वंचितों की आबादी के बीच से भी कुछ जजों को न्यायालयों में स्थान मिलेगा मगर ऐसा नहीं हुआ। स्थिति कितनी चिंताजनक है यह ऊपर के आंकड़ों से पता चल गया होगा। यह अकारण नहीं कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण के लम्बित मामलों की जल्द सुनवाई हेतु एक अपील जब सर्वोच्च न्यायालय में जाती है तो उसे स्वीकार करने या नकारने के बजाए, जज महोदय याचिकाकर्त्ता पर दस लाख का जुर्माना ठोंक देते हैं। यह जुर्माना, उस मानसिकता का द्योतक है जो दर्शाता है कि वंचितों को अपने हितों की मांग नहीं करनी चाहिए।
यह याचिका अकारण नहीं आई थी। दूसरे वर्ग के जजों द्वारा ज्यादातर फैसले वंचितों के हितों के विरुद्ध देखे गए हैं और वहीं ई.डब्लू.एस. मामले में न्यायालय का विभाजित फैसला इस तरह आया जो मूलतः सवर्ण हितों का पोषक रहा।
विगत एक दशक में न्यायालयों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं आया है जो वंचितों के हितों की हिफाजत करता हो। खासकर आरक्षण के मामले में इतना घालमेल कर दिया गया है कि ओबीसी, एस.सी., एस.टी. की भागीदारी का मार्ग अवरुद्ध होने लगा है। संविधान के प्राविधानों के विरुद्ध लाया गया ई.डब्लू.एस. बरकरार ही नहीं है, उसका प्रतिशत बिना किसी आधार के बढ़ा दिया जा रहा है। कहा गया था कि सामान्य सीटों के अंतर्गत ही यह दस प्रतिशत की सीमा में रहेगा मगर कहीं-कहीं तो यह ओ.बी.सी. सीटों के बराबर चला जा रहा है।
सामान्य सीटों का मामला तमाम फैसलों के बावजूद, ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के लिए मनमाने तरीके से परिभाषित हो रहा है और ज्यादातर मामलों में सामान्य सीटों को, सवर्ण सीट मान लिया जाता है। साक्षात्कारों में सवर्ण बहुमत की पक्षधरता अलग हितसाधक बनी हुई है। कुल मिलाकर न्यायालयों की वंचित विरोधी मानसिकता ने वंचितों को किनारे लगाना शुरू कर दिया है। न्याय एक परिकल्पित शब्द बनकर रह गया है। मणिपुर के धधकाने और महिलाओं की आबरू लूटे जाने के पीछे, उच्च न्यायालय का वंचित विरोधी फैसला मूल में है।
जब तक सभी सामाजिक समुदायों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में नियुक्तियां नहीं होंगी या जिस अनुपात में कम नियुक्तियां होंगी उसी अनुपात में उनके साथ भेदभाव और अन्याय होता रहेगा। सामाजिक अन्याय और न्याय का यही समाजशास्त्र है। यह बात, देश के कुल संसाधनों पर कब्जा बनाए रखने, नियुक्तियों में पद हथियाने, अपराधों में अपराधियों को बचाने, न्यायिक फैसलों की न्यायप्रियता, आर्थिक विषमताओं का बढ़ाने, ज्ञान और अज्ञान के फासलों को बनाए रखने, आदि में दिखाई देती रहेगी। इसलिए वक्त का तकाजा है कि लोकतंत्र की बुनियाद बचाने और समतामूलक शासन को स्थापित करने के लिए न्यायिक तंत्र में वंचितों की समुचित उपस्थिति दर्ज हो।
(सुभाष चन्द्र कुशवाहा इतिहासकार और साहित्यकार हैं।)